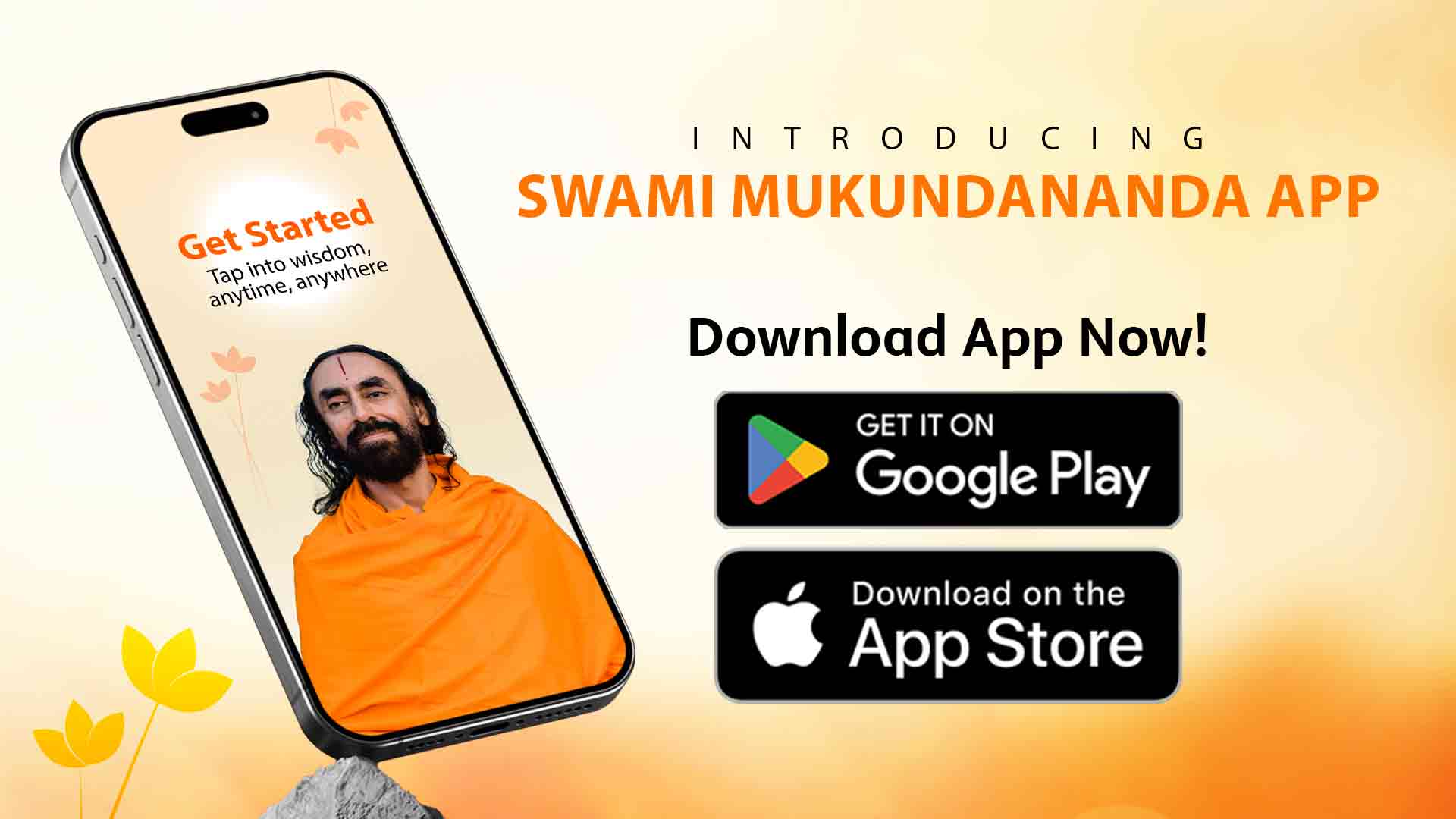श्रीमद्भागवत महापुराण- स्कन्ध: 7 अध्याय: 1-3
राजा परीक्षित् ने शुकदेवजी से प्रश्न किया कि भगवान् तो समदर्शी, निष्पक्ष, सबके प्रिय और कल्याणस्वरूप हैं, फिर वे इन्द्र जैसे देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों का वध क्यों करते हैं? जबकि वे न तो देवताओं के मोह में हैं, न दैत्यों से द्वेष करते हैं, क्योंकि वे तो निर्गुण और पूर्ण हैं।
इसपर शुकदेवजी ने कहा कि यह प्रश्न बहुत सुंदर और भक्तिपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान् की लीला और उनके भक्तों की महिमा का रहस्य छिपा है। यह कथा नारद आदि महात्मा प्रेम से गाते हैं और इससे भक्ति बढ़ती है। वास्तव में भगवान् अजन्मा, निर्गुण और प्रकृति से परे हैं। लेकिन जब वे लीला करते हैं, तो अपनी माया से सत्त्व, रज और तम — इन गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। ये गुण परमात्मा के नहीं, प्रकृति के हैं। समय के अनुसार इन गुणों की वृद्धि होती है:
- सत्त्वगुण के समय वे देवताओं और ऋषियों का सहारा लेते हैं,
- रजोगुण के समय दैत्यों का,
- और तमोगुण के समय यक्षों व राक्षसों का।
परमात्मा तो सबमें व्याप्त हैं, जैसे अग्नि काष्ठ में छिपी रहती है। लेकिन जब वे लीला हेतु शरीर धारण करते हैं, तो माया के अनुसार गुणों की रचना करते हैं — रमण के लिए सत्त्व, निर्माण के लिए रज, और विश्राम के लिए तम। भगवान् स्वयं काल के अधीन नहीं, बल्कि काल भी उनके अधीन है। जब वे सत्त्वगुण की वृद्धि करते हैं, तो देवताओं का कल्याण और दैत्यों का विनाश होता है — यह उनका समभाव ही है, क्योंकि वे सभी प्राणियों के आत्मस्वरूप हैं।
शुकदेवजी ने बताया कि एक बार देवर्षि नारदजी ने भी इसी विषय पर एक अद्भुत प्रसंग सुनाया था, जब तुम्हारे पितामह युधिष्ठिर ने उनसे राजसूय यज्ञ के समय एक प्रश्न किया था। उस यज्ञ में एक चमत्कार हुआ—चेदिराज शिशुपाल, जो जीवन भर भगवान श्रीकृष्ण की निंदा करता रहा, यज्ञ सभा में सबके सामने श्रीकृष्ण में ही लीन हो गया। यह देखकर युधिष्ठिर चकित रह गये। वे समझ नहीं पाए कि श्रीकृष्ण जैसे परब्रह्म में लीन होना तो अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, फिर वह निंदक शिशुपाल कैसे उस परम गति को प्राप्त हुआ?
युधिष्ठिर ने पूछा—शिशुपाल और दन्तवक्त्र जैसे लोग तो बचपन से ही श्रीकृष्ण से द्वेष करते रहे, उनकी निंदा करते रहे, पर न तो उन्हें कोई कष्ट मिला, न ही कोई पापकर्म का दंड। उल्टे वे तो वही परम गति प्राप्त कर गये, जो महाभक्तों को भी कठिनता से मिलती है। ऐसा क्यों?
युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि पहले तो भगवान की निंदा करने पर राजा वेन को ऋषियों ने नरक में भेज दिया था। फिर यह अपवाद क्यों?
युधिष्ठिर के प्रश्नों से प्रसन्न होकर देवर्षि नारदजी ने सबके सामने एक गूढ़ रहस्य बतलाया। उन्होंने कहा कि शिशुपाल और दन्तवक्त्र, जो जीवनभर श्रीकृष्ण का अपमान करते रहे, वास्तव में वैकुण्ठ के द्वारपाल जय और विजय थे। उन्हें सनकादि ऋषियों के शाप के कारण तीन जन्मों तक पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा।
नारदजी ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण जैसे पूर्ण ब्रह्म में चिंतन चाहे प्रेम, भक्ति, भय, द्वेष, कामना या स्नेह से हो, यदि मन उनमें एकाग्र हो जाए, तो जीव उन्हें प्राप्त कर सकता है। शिशुपाल और दन्तवक्त्र ने द्वेषवश लगातार श्रीकृष्ण का स्मरण किया, इसी कारण अंत में उनका उद्धार हो गया।
इसके पूर्व जन्मों में ये:
- हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने—भगवान वराह और नृसिंह ने उनका वध किया।
- फिर रावण और कुम्भकर्ण बने—भगवान राम ने उन्हें मारा।
- अंत में शिशुपाल और दन्तवक्त्र बने—भगवान श्रीकृष्ण ने उनका वध किया।
तीनों बार उनका भगवान से द्वेषपूर्ण चिन्तन रहा, पर वह भी अंततः उद्धार का कारण बना। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा कि हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद जैसे भक्त पुत्र से इतना द्वेष क्यों किया, और प्रह्लाद को भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हुई?
हिरण्यकशिपु का तत्व-ज्ञान
नारदजीने कहा-युधिष्ठिर! जब भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, तब उसका भाई हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गया। वह गुस्से से काँपने लगा, दाँत पीसने लगा और अपनी सेना के प्रमुख दैत्यों व राक्षसों को इकट्ठा करके आदेश दिया।
उसने कहा कि विष्णु ने छल से उसके प्रिय भाई की हत्या की है, अब वह विष्णु का गला काटकर अपने भाई का तर्पण करेगा। उसने विष्णु को मायावी और पक्षपाती कहा और संकल्प लिया कि पहले विष्णु का अंत करेगा, जिससे देवता भी स्वतः नष्ट हो जाएँगे। फिर हिरण्यकशिपु ने अपने अनुयायियों को आज्ञा दी कि वे पृथ्वी पर जाकर यज्ञ, तप, वेद, धर्म और ब्राह्मणों को नष्ट करें—क्योंकि वही विष्णु की शक्ति और आधार हैं। जहाँ भी धर्म और पुण्य का कार्य हो रहा हो, वहाँ विनाश कर दो।
दैत्य भी अपने स्वभाववश अत्याचार करने लगे। उन्होंने नगर, गाँव, खेत, जंगल, आश्रम, व्यापारिक स्थल, गायों के स्थान, किसानों की बस्तियाँ—सभी को उजाड़ डाला और आग लगा दी। फलस्वरूप धरती पर हाहाकार मच गया, धर्म का नाश होने लगा और देवता भी स्वर्ग छोड़कर छिपते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे।
उस समय राक्षसों के कई प्रमुख—जैसे शकुनि, शम्बर, वृक, महानाभ, आदि—उसके पुत्रों और परिवार को सांत्वना देने आए। हिरण्यकशिपु ने अपनी माता दिति, अपने भाई की पत्नी रुषाभानु और अपने भतीजों से सांत्वना-पूर्वक कहा—“वीरों की मृत्यु युद्धभूमि में ही शोभा देती है। इसलिए हिरण्याक्ष की मृत्यु कोई शोक का कारण नहीं है।”
फिर उसने जीवन, आत्मा और मृत्यु के गहरे रहस्यों की बात की। उसने समझाया:
- आत्मा नित्य (शाश्वत), अविनाशी, शुद्ध और सर्वज्ञ है।
- यह शरीर और मन से अलग है, लेकिन अज्ञानवश आत्मा को शरीर से एकत्व मान लिया जाता है—यही दुखों की जड़ है।
- जैसे बहती जलधारा में प्रतिबिंब हिलता-सा दिखता है, वैसे ही मन की चंचलता के कारण आत्मा को भी चंचल और भटकता हुआ समझा जाता है।
- प्रिय-अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछुड़ना, जन्म-मृत्यु, दुःख, मोह सब अज्ञान (अविद्या) के उपज हैं।
ततरी की कथा और यम का संदेश
फिर हिरण्यकशिपु ने आगे कहा कि इस विषय में एक प्राचीन कथा कहता है। उशीनर देश के यशस्वी और पराक्रमी राजा सुयज्ञ युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। उनका शरीर घायल, धूल-धूसरित और अस्त्र-शस्त्रों से बिखरा पड़ा होता है। उनका सौम्य चेहरा अब मृत्यु से विकृत हो चुका होता है। उनके भाई-बन्धु और सैनिक उनका शव घेरकर खड़े हो जाते हैं।
राजा की रानियाँ जब यह दृश्य देखती हैं, तो वे दुःख से पागल हो जाती हैं। छाती पीटती हैं, विलाप करती हैं — “हाय नाथ! आपने हमें छोड़ दिया। अब हम किसके सहारे जियेंगी? आप तो हमारी सेवा से सन्तुष्ट रहते थे, अब हमें अपने साथ ले चलें।” वे अपने प्राणनाथ के चरणों में गिर पड़ती हैं और रोते-रोते उनके पवित्र चरण आँसुओं से भीग जाते हैं। रानियों का यह करुण क्रंदन पूरे वातावरण को विषाद से भर देता है।
उसी समय, वहाँ यमराज एक बालक के रूप में प्रकट होते हैं। वे सबके शोक और मूढ़ता को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, "तुम सब तो बड़े समझदार हो, फिर भी मृत्यु पर शोक कर रहे हो? जिसे तुम ‘सुयज्ञ’ कहते हो, उसका शरीर तो यहीं पड़ा है। पर जिसमें चेतना थी, जो सुनता-बोलता था — वह आत्मा तो अब यहाँ नहीं है। तुम कभी आत्मा को नहीं देख पाए, तो अब उसके न दिखने पर इतना विलाप क्यों?"
वे समझाते हैं कि आत्मा नित्य, अविनाशी, अजर और अमर है। शरीर एक मिट्टी का पुतला है, जैसे घर एक ढांचा होता है — वैसे ही यह देह है। आत्मा केवल देह में अस्थायी रूप से वास करती है। जैसे सोने से बने आभूषण बदलते रहते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। वे कहते हैं कि:
- जो आत्मा है, वह वायु की तरह देह में रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं होती।
- जो जन्म लेता है, उसका मरना निश्चित है। फिर शोक क्यों?
- मृत्यु तो केवल पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। न कोई जल्दी मरेगा, न देर से।
- भाग्य के अनुसार ही सब कुछ घटित होता है — न ज़रा ज़्यादा, न ज़रा कम।
यमराज एक कथा सुनाते हैं — एक बहेलिया एक बार एक कुलिंग पक्षी (ततरी) के जोड़े को फँसाता है। मादा पक्षी जाल में फँस जाती है, और नर पक्षी उसकी पीड़ा देख विलाप करता है, दुःखी होता है और अपने बच्चों की चिंता करता है। परन्तु अन्त में वह भी बहेलिए के बाण से मारा जाता है। इस उदाहरण से यमराज समझाते हैं — “मूर्ख रानियो! तुम्हारी भी यही दशा होनेवाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दीखती नहीं और इसके लिये रो-पीट रही हो! यदि तुमलोग सौ बरसतक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो, तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी।”
हिरण्यकशिपुने कहा-उस छोटेसे बालककी ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सब-के-सब दंग रह गये। उशीनर-नरेशके भाई-बन्धु और स्त्रियोंने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख-दुःख अनित्य एवं मिथ्या हैं। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहीं अन्तर्धान हो गये। भाई-बन्धुओंने भी सुयज्ञकी अन्त्येष्टि-क्रिया की। इसलिये तुमलोग भी अपने लिये या किसी दूसरेके लिये शोक मत करो। इस संसारमें कौन अपना है और कौन अपनेसे भिन्न? क्या अपना है और क्या पराया? प्राणियोंको अज्ञानके कारण ही यह अपनेपरायेका दुराग्रह हो रहा है, इस भेद-बुद्धिका और कोई कारण नहीं है। अपनी पुत्रवधूके साथ दितिने हिरण्यकशिपुकी यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्रशोकका त्याग कर दिया और अपना चित्त परमतत्त्वस्वरूप परमात्मामें लगा दिया।
हिरण्यकशिपु की भयानक तपस्या और अमरता का असंभव वर
नारदजी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने ठान लिया कि वह अजेय, अजर, अमर और त्रिलोकी का एकछत्र सम्राट बनेगा — ऐसा कि कोई उसके सामने खड़ा तक न हो सके। इस उद्देश्य से वह मन्दराचल पर्वत की एक गुफा में कठोर तपस्या करने लगा। वह अंगूठे के बल खड़ा होकर हाथ ऊपर उठाए, आकाश की ओर देखता हुआ हजारों वर्षों तक तप करता रहा। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि उसके शरीर से निकली गर्मी की ज्वाला पूरे ब्रह्मांड को जलाने लगी— नदियाँ, समुद्र खौल उठे, पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाएँ जलने लगीं और स्वर्ग तक असहनीय हो गया।
देवता घबराकर ब्रह्माजी के पास जाकर बोले कि हिरण्यकशिपु ब्रह्माजी जैसा सर्वोच्च पद पाना चाहता है और धर्म की व्यवस्था पलट देना चाहता है। वे समय रहते इसे रोके, वरना तीनों लोकों में संकट आ जाएगा। जब देवताओं ने ब्रह्माजी से प्रार्थना की, तो वे प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के तपस्थल पर पहुँचे।
वहाँ उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु का शरीर दीमक, घास और बाँसों से ढँका हुआ था—उसकी त्वचा, माँस और रक्त चींटियाँ चाट चुकी थीं। फिर भी उसकी तपस्या की ज्वाला से तीनों लोक तप रहे थे। ब्रह्माजी स्वयं आश्चर्यचकित हुए और मुस्कराते हुए बोले—"बेटा हिरण्यकशिपु! तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। तुम्हारी इच्छानुसार मैं वर देने आया हूँ। तुम्हारा यह तप असाधारण है—ना पहले किसी ने ऐसा किया, ना आगे करेगा। तुमने मुझे वश में कर लिया है।" यह कहकर ब्रह्माजी ने अपने कमंडल का दिव्य जल उसके शरीर पर छिड़का। तुरंत वह जल छूते ही हिरण्यकशिपु नवयुवक बनकर उठ खड़ा हुआ—उसका शरीर शक्तिशाली, इन्द्रियाँ प्रखर और रूप स्वर्ण जैसा दमकता हुआ था।
हिरण्यकशिपु ने ब्रह्माजी को सामने देखकर अत्यन्त भावुक होकर साष्टांग प्रणाम किया और गद्गद वाणी से स्तुति करने लगा। उसने कहा—आप ही इस त्रिगुणमय जगत के रचयिता, पालक और संहारक हैं। समस्त ज्ञान, विज्ञान, वेद, यज्ञ, प्राण, मन और इन्द्रियाँ आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप काल, आत्मा और ब्रह्मस्वरूप हैं, जो साकार और निराकार दोनों रूपों में सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। यह ब्रह्माण्ड भी आपके गर्भ से ही प्रकट हुआ है।
यदि दास्यस्यभिमतान्वरान्मे वरदोत्तम। भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो ।
नान्तर्बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधैः। न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि ।
व्यसुभिर्वासुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः। अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनाम् ।
प्रभो! आप समस्त वरदाताओंमें श्रेष्ठ हैं। यदि आप मझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं, तो ऐसा वर दीजिये कि आपके बनाये हुए किसी भी प्राणीसे–चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नागादि किसीसे भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर-बाहर, दिनमें, रात्रिमें, आपके बनाये प्राणियोंके अतिरिक्त और भी किसी जीवसे, अस्त्र-शस्त्रसे, पृथ्वी या आकाशमें कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्धमें कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियोंका एकच्छत्र सम्राट होऊँ।(भागवत 7.3.35-37)
सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः। तपोयोगप्रभावाणां यन्न रिष्यति कर्हिचित्।
इन्द्रादि समस्त लोकपालोंमें जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियोंको जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे भी दीजिये। (भागवत 7.3.38)
नारदजी कहते हैं-युधिष्ठिर! जब हिरण्यकशिपुने ब्रह्माजीसे इस प्रकारके अत्यन्त दुर्लभ वर माँगे, तब उन्होंने उसकी तपस्यासे प्रसन्न होनेके कारण उसे वे वर दे दिये। ब्रह्माजीने कहा-बेटा! तुम जो वर मुझसे माँग रहे हो, वे जीवोंके लिये बहुत ही दुर्लभ हैं; परन्तु दुर्लभ होनेपर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिये देता हूँ।
सारांश: JKYog India Online Class- श्रीमद् भागवत कथा [हिन्दी]- 02.05.2025