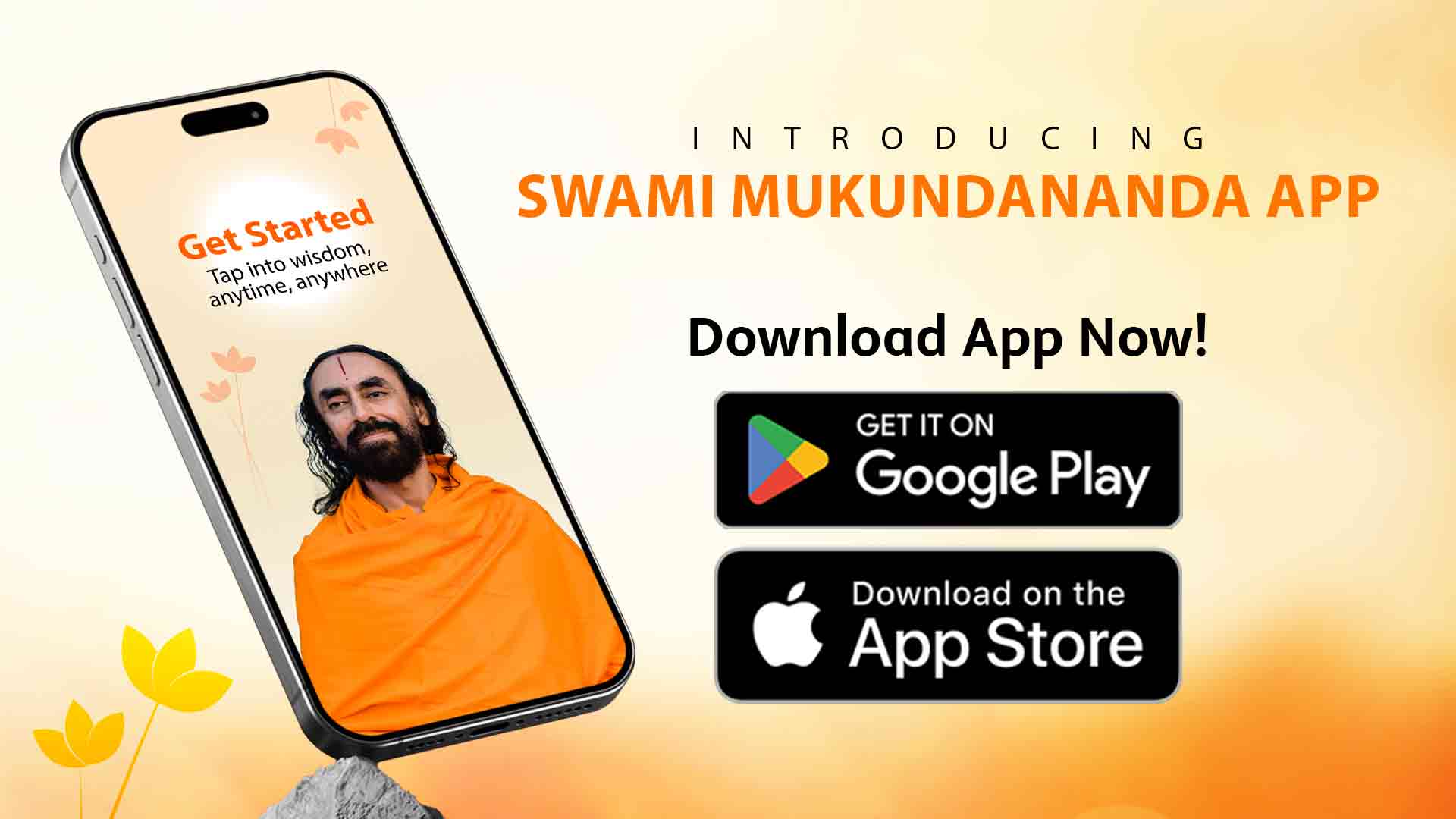श्रीमद्भागवत महापुराण- स्कन्ध: 7 अध्याय: 10-11
नारदजी युधिष्ठिर से कहते हैं — 'हे राजन्! तुमने मुझसे यह जिज्ञासा की थी कि वे शिशुपाल आदि, जो भगवान से द्वेष रखते थे, उन्हें भगवान के समान स्वरूप — अर्थात् सारूप्य मुक्ति — कैसे प्राप्त हुई? अब मैं उसका उत्तर तुम्हें दे चुका हूँ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, फिर रावण और कुम्भकर्ण, और अंततः शिशुपाल तथा दन्तवक्त्र — इन सभी ने श्रीकृष्ण से सारा जीवन वैरभाव रखा एवं मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी इनका चित्त केवल श्रीकृष्ण में ही लीन था। उसी निरंतर चिंतन के प्रभाव से वे भगवान के ही स्वरूप को प्राप्त हो गए। यह ठीक वैसे ही है जैसे भृंगी नामक कीट किसी सामान्य कीड़े को पकड़कर अपने बिल में बंद कर देता है। भय के कारण वह कीड़ा निरंतर उसी भृंगी का चिंतन करता रहता है, और अंततः उसका स्वरूप ही धारण कर लेता है। इस प्रकार चाहे प्रेमभाव से हो या वैरभाव से — यदि चिंतन निरंतर भगवद्मय हो जाए, तो वही मोक्ष का कारण बन जाता है।'
नारदजी आगे कहते हैं की जो मनुष्य एकाग्रचित्त से परम पुरुष परमात्मा की श्रीनृसिंह लीला, हिरण्यकशिपु वध, और प्रह्लादजी की भक्ति, ज्ञान और प्रभाव को पढ़ता और सुनता है, वह भगवान के अभय पद – वैकुण्ठधाम – को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर! इस मनुष्यलोक में तुम लोगों का भाग्य अत्यन्त प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण मनुष्य का रूप लेकर गुप्तरूप से निवास करते हैं। यही कारण है कि संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाले ऋषि-मुनि बार-बार उनके दर्शन हेतु तुम्हारे पास आते रहते हैं। जिन परमात्मा को बड़े-बड़े महापुरुष निरन्तर खोजते रहते हैं, जो माया से रहित, परम शान्ति और परमानन्द स्वरूप हैं—वे ही तुम्हारे प्रिय, हितैषी, सखा, पूज्य, आज्ञाकारी, गुरु और आत्मस्वरूप श्रीकृष्ण हैं। शंकर, ब्रह्मा आदि देवता भी अपनी पूरी बुद्धि लगाकर यह नहीं कह सके कि "वे ऐसे हैं", तो हम जैसे साधारण जन उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं? हम तो केवल मौन, भक्ति और संयम के माध्यम से ही उनकी पूजा करते हैं। हमारी यह पूजा वे कृपापूर्वक स्वीकार करें और भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्ण हम पर प्रसन्न हों। प्राचीन काल में मायावी मयासुर ने जब भगवान रुद्र की कीर्ति को कलंकित करना चाहा, तब श्रीकृष्ण ने उनकी यश की रक्षा की और उसे बढ़ाया।
यह सुनकर युधिष्ठिर ने नारदजी से पूछा—"मयासुर किस कार्य से रुद्रजी का यश नष्ट करना चाहता था और श्रीकृष्ण ने उसे कैसे बचाया? कृपया बताइये।"
नारदजीने कहा-एक बार इन्हीं भगवान् श्रीकृष्णसे शक्ति प्राप्त करके देवताओंने युद्धमें असुरोंको जीत लिया था। उस समय सब-के-सब असुर मायावियोंके परमगुरु मयदानवकी शरणमें गये। शक्तिशाली मयासुरने सोने, चाँदी और लोहेके तीन विमान बना दिये। वे विमान क्या थे, तीन पुर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना-जाना जान नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियाँ भरी हुई थीं। दैत्य सेनापति पहले से ही तीनों लोकों और देवताओं से द्वेष रखते थे। अब वे इन विमानों में छिपकर सभी को नष्ट करने लगे। इससे परेशान होकर सारे देवता और लोकपाल भगवान शंकर के पास पहुँचे और बोले, "प्रभो! त्रिपुर में रहने वाले असुर हमें मार रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा करें।"
शंकरजी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और कहा, "डरो मत।" फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर त्रिपुर (तीनों पुरों) पर चला दिया। उस बाण से सूर्य की किरणों जैसी अग्नि लपटें निकलने लगीं और विमानों का सब कुछ ढक गया।
बाणों के प्रभाव से असुर मरकर गिरने लगे। लेकिन मयासुर तो बहुत मायावी था—वह उन्हें उठाकर अपने बनाए अमृत के कुएँ में डालने लगा। उस अमृत को छूते ही असुर फिर से ज़िंदा हो गए और पहले से भी ज़्यादा तेजस्वी और मजबूत होकर उठ खड़े हुए।
भगवान् श्रीकृष्णने जब देखा कि महादेवजी तो अपना संकल्प पूरा न होनेके कारण उदास हो गये हैं, तब उन असुरोंपर विजय प्राप्त करनेके लिये इन्होंने एक युक्ति की। भगवान् विष्णु उस समय गौ बन गये और ब्रह्माजी बछड़ा बने। दोनों ही मध्याह्नके समय उन तीनों पुरोंमें गये और उस सिद्धरसके कुएँका सारा अमृत पी गये। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनोंको देख रहे थे, फिर भी भगवान्की मायासे वे इतने मोहित हो गये कि इन्हें रोक न सके। जब मयासुरको यह बात मालूम हुई, तब भगवान्की इस लीलाका स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करनेवाले अमृत-रक्षकोंसे उसने कहा-‘भाई! देवता, असुर, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने, पराये अथवा दोनोंके लिये जो प्रारब्धका विधान है, उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था, हो गया। शोक करके क्या करना है?’
इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से भगवान शंकर के युद्ध के लिए सारी सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथि, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अन्य शक्तियों से अन्य आवश्यक वस्तुओं का निर्माण किया। इन दिव्य सामग्रियों से सजकर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए और धनुष-बाण धारण किए। अभिजित मुहूर्त में उन्होंने बाण चढ़ाया और तीनों अजेय विमानों (त्रिपुरों) को भस्म कर दिया। उसी समय स्वर्ग में दुन्दुभियाँ बजने लगीं, देवता, ऋषि, पितर और सिद्धगण आनन्द से जयजयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएँ नाचने-गाने लगीं। इस प्रकार तीनों पुरों का संहार करके भगवान शंकर ने ‘पुरारि’ (पुरों के संहारक) की उपाधि प्राप्त की और ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति सुनते हुए अपने धाम लौट गये। नारदजी यह कथा सुनते हुए कहते हैं, "भगवान श्रीकृष्ण ही इस समस्त लीला के कर्ता हैं। वे अपनी माया से मनुष्यों के समान लीला करते हैं, और ऋषिगण उन्हीं की लोकपावन लीलाओं का गान करते हैं। बताओ युधिष्ठिर! अब तुम्हें मैं और क्या सुनाऊँ?"
वर्ण और आश्रमों के अनुसार मनुष्यों का सनातन धर्म क्या है?
श्री शुकदेवजी कहते हैं कि जब प्रह्लादजी का पावन चरित्र युधिष्ठिर ने नारदजी से सुना, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने नारदजी से और प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर ने कहा—"भगवन्! अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि वर्ण और आश्रमों के अनुसार मनुष्यों का सनातन धर्म क्या है। क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत्प्रेम और अंत में परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप तो स्वयं ब्रह्माजी के पुत्र हैं, और आपकी तपस्या, योग और समाधि इतनी महान है कि ब्रह्माजी भी आपको अपने अन्य पुत्रों से अधिक मानते हैं। आप धर्म के गूढ़ रहस्यों को जितनी स्पष्टता से जानता है, उतनी और कोई नहीं जानता।"
इस पर नारदजी बोले—"युधिष्ठिर! सभी धर्मों का मूल तो स्वयं अजन्मा भगवान ही हैं। वे ही समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और मूर्ति के पुत्र के रूप में अपने अंश से अवतरित होकर बदरिकाश्रम में तप कर रहे हैं। मैं उन्हीं भगवान नारायण को नमस्कार करके, उनके मुख से सुना हुआ सनातन धर्म अब तुम्हें सुनाता हूँ।"
धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः ।
स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति ॥
युधिष्ठिर! सर्ववेदस्वरूप भगवान् श्रीहरि, उनका तत्त्व जाननेवाले महर्षियोंकी स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्मप्रसादकी उपलब्धि हो, वह कर्म धर्मके मूल हैं। (भागवत 7.11.7)
धर्मके ये तीस लक्षण
सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः ।
अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥
सन्तोषः समदृक् सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः ।
नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनं आत्मविमर्शनम् ॥
अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः ।
तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव ॥
श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः ।
सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्म समर्पणम् ॥
नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः ।
त्रिंशत् लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति ॥
युधिष्ठिर! शास्त्रों में धर्म के तीस लक्षण बताए गए हैं, जो हर मनुष्य के लिए श्रेष्ठ मार्ग हैं। ये लक्षण हैं: (1) सत्य बोलना, (2) दया रखना, (3) तपस्या करना, (4) शौच अर्थात् आंतरिक और बाह्य शुद्धता, (5) तितिक्षा यानी कष्ट सहने की शक्ति, (6) उचित और अनुचित का विवेक, (7) मन का संयम, (8) इन्द्रियों का संयम, (9) अहिंसा का पालन, (10) ब्रह्मचर्य, (11) त्याग की भावना, (12) स्वाध्याय, (13) सरल स्वभाव, (14) संतोष, (15) समदर्शी महात्माओं की सेवा, (16) धीरे-धीरे भोगों की इच्छा से निवृत्ति, (17) यह विचार कि अहंकार से किया गया प्रयास उलटा फल देता है, (18) मौन और आत्मचिंतन, (19) प्राणियों में अन्न आदि का उचित वितरण, (20) सभी में विशेष रूप से मनुष्यों में आत्मा और इष्टदेव का भाव देखना, (21) संतों की शरण में जाना, (22) भगवान श्रीकृष्ण के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, (23) कीर्तन, (24) स्मरण करना, (25) सेवा, (26) पूजन, (27) नमस्कार करना, (28) भगवान के प्रति दास्य भाव रखना, (29) सख्य भाव से जुड़ना और (30) आत्मसमर्पण करना। इन तीसों प्रकार के आचरणों को अपनाने से सर्वात्मा भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। यही सभी मनुष्यों का परम धर्म है। (भागवत 7.11.8-12)
द्विज जाती के कर्म एवं आजीविका के साधन
धर्मराज युधिष्ठिर से नारदजी ने कहा कि जिनके कुल में सदैव संस्कार हुए हों उन्हें द्विज (द्विजाति) कहा जाता है। इन द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य जैसे कर्म निर्धारित हैं।
ब्राह्मण के लिए छह कर्म (1) अध्ययन, (2) अध्यापन, (3) यज्ञ करना, (4) यज्ञ कराना, (5) दान देना और (6) दान लेना बताए गए हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए; उसका जीवन कर, जुर्माना आदि से चलता है। वैश्य को खेती, गौ-रक्षा और व्यापार द्वारा जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है सेवा प्रदान करना।
ब्राह्मणों की आजीविका के चार साधन बताए गए हैं: (1) वर्ता- व्यापार, कृषि, गोरक्षा, या अन्य व्यावसायिक उपार्जन के साधन, (2) शालीन- शास्त्राध्ययन व शिक्षण, यज्ञ, और दान पर आधारित जीवन, (3) यायावर- भिक्षा माँगकर या घूम-घूमकर जीविका और (4) शिलोञ्छन- खेत में गिरे हुए अन्न के दानों से निर्वाह। इनमें अंतिम साधन सबसे श्रेष्ठ है।
निम्न वर्ण का व्यक्ति बिना आपातकालीन परिस्थिति के उच्च वर्ण की आजीविका नहीं अपनाए। हां, आपातकालीन परिस्थिति के समय कोई भी सब प्रकार की वृत्तियाँ अपना सकता है। ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत–इनमेंसे किसी भी वृत्तिका आश्रय ले, परन्तु श्वानवृत्तिका अवलम्बन कभी न करे।
- ऋत: बाजारमें पड़े हुए अन्न (उञ्छ) तथा खेतोंमें पड़े हुए अन्न (शिल)-को बीनकर ‘शिलोञ्छ’ वृत्तिसे जीविका-निर्वाह करना ‘ऋत’ है।
- अमृत: बिना माँगे जो कुछ मिल जाय, उसी अयाचित (शालीन) वृत्तिके द्वारा जीवन-निर्वाह करना ‘अमत’ है।
- मृत: नित्य माँगकर लाना अर्थात् ‘यायावर’ वृत्तिके द्वारा जीवन-यापन करना ‘मृत’ है।
- प्रमृत: कृषि आदिके द्वारा ‘वार्ता’ वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करना ‘प्रमृत’ है।
- सत्यानृत: वाणिज्य ‘सत्यानृत’ है और
- श्वानवृत्ति: निम्नवर्णकी सेवा करना ‘श्वानवृत्ति’ है।
शमो दमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम् ।
ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम् ॥
शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत्परायणता और सत्य–ये ब्राह्मणके लक्षण हैं। (भागवत 7.11.21)
शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजः त्याग आत्मजयः क्षमा ।
ब्रह्मण्यता प्रसादश्च सत्यं च क्षत्रलक्षणम् ॥
युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजाको रक्षा करना-ये क्षत्रियके लक्षण हैं। (भागवत 7.11.22)
देवगुर्वच्युते भक्तिः त्रिवर्गपरिपोषणम् ।
आस्तिक्यं उद्यमो नित्यं नैपुण्यं वैश्यलक्षणम् ॥
देवता, गुरु और भगवान्के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम-इन तीनों पुरुषार्थोंकी रक्षा करना; आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यावहारिक निपुणता-ये वैश्यके लक्षण हैं। (भागवत 7.11.23)
शूद्रस्य सन्नतिः शौचं सेवा स्वामिन्यमायया।
अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गोविप्र रक्षणम् ॥
विनम्रता, शुद्धता, सेवा, स्वामी आश्रय, कुशल व्यवहार, मंत्रों के बिना यज्ञ करना, चोरी न करना, सत्य बोलना, और गो-विप्र रक्षण शुद्र के लक्षण हैं। (भागवत 7.11.24)
वेदों के जानकार ऋषि-मुनियों ने युगों-युगों से मनुष्यों के स्वभाव को ध्यान में रखकर उनके लिए धर्म की व्यवस्था की है। यही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक दोनों में कल्याणकारी होता है। जो व्यक्ति अपने स्वाभाविक स्वधर्म का पालन करता है, वह धीरे-धीरे अपनी वासनाओं और गुणों से ऊपर उठ सकता है। जैसे ज़मीन को बार-बार बोने से वह थक जाती है और अंत में बीज उगने भी बंद हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का चित्त भी विषय-भोगों से अंततः ऊब जाता है। थोड़े-थोड़े भोग मन को लालची बनाए रखते हैं, परंतु जब विषयों की अधिकता हो जाती है, तो मन उनसे भी ऊबकर विरक्त हो सकता है — जैसे घी की बूंदों से आग जलती रहती है, लेकिन अचानक ज़्यादा घी डाल देने पर वह बुझ जाती है।
यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम् ।
यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत्॥
जिस पुरुषके वर्णको बतलानेवाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्णवालेमें भी मिले तो उसे भी उसी वर्णका समझना चाहिये। (भागवत 7.11.35)
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणै: ।।
हे शत्रुहंता! ब्राह्मणों, श्रत्रियों, वैश्यों और शुद्रों के कर्तव्यों को इनके गुणों के अनुसार तथा प्रकृति के तीन गुणों के अनुरूप वितरित किया गया है, न कि इनके जन्म के अनुसार। (गीता 18.41)
कलियुग का धर्म
सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों में वर्णाश्रम धर्म का पालन अपेक्षाकृत सहज था, क्योंकि उन युगों में मनुष्य की तपश्चर्या, संयम, सत्यनिष्ठा और आयु सभी उच्च स्तर की होती थी। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट था, और आत्मकल्याण की भावना समाज में व्याप्त थी। किंतु कलियुग में यह व्यवस्था केवल ग्रंथों में ही शेष रह गई है — व्यवहार में लगभग लुप्तप्राय हो गई है। इसका कारण यह है कि जन्म से ही मनुष्यों की प्रवृत्तियाँ विकृत और असंयमित होती जा रही हैं; संयम और तप की शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई है; धर्म के प्रति श्रद्धा और जिज्ञासा समाज में दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है; और अधिकांश लोग अपने कर्मों के यथार्थ फल को जानना भी नहीं चाहते। फलतः आज के युग में वर्णाश्रम धर्म का पालन न तो सहज है, न ही व्यवहारिक और अधिकतर स्थानों पर इसका दुरुपयोग ही होता है। इन्हीं सभी दोषों को देखकर शास्त्रों में कलियुग में मनुष्य के कल्याण के लिए दान एवं हरि नाम संकीर्तन को कल्याण का प्रमुख माध्यम बताया गया है, न कि धर्म, कर्म, यज्ञ इत्यादि को।
श्री चैतन्य-चरितामृत
हरेर नाम हरेर नाम हरेर नमैव केवलम I
कलौ नस्ति एव नस्ति एव नस्ति एव गतिर् अन्यतः II
कलियुग में केवल हरि नाम का ही आश्रय है। इस युग में न तो कोई अन्य मार्ग है, न ही कोई अन्य उपाय- केवल हरि नाम संकीर्तन ही कल्याण का एकमात्र साधन है।
श्रीरामचरितमानस
कलिजुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना। एक अधार राम गुन गाना॥
सब भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि॥
कलियुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री रामजी का गुणगान ही एकमात्र आधार है।
श्रीमद् भागवत महापुराण
कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान् गुण: ।
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्ग: परं व्रजेत् ॥
हे राजन्! कलियुग दोषों का महासागर है, लेकिन इसमें एक महान गुण भी है- कि केवल श्रीकृष्ण के नाम का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सब बंधनों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सकता है।
कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै: ।
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात् ॥
सत्य युग में भगवान विष्णु की उपासना ध्यान (तपस्या) के द्वारा होती है, त्रेता युग में यज्ञों के माध्यम से,
द्वापर युग में पूजा-अर्चना और विधिपूर्वक सेवा के द्वारा, और कलियुग में वही भगवान केवल नाम संकीर्तन (नाम जप और भजन) से प्राप्त होते हैं।
द्वापर युग में पूजा-अर्चना और विधिपूर्वक सेवा के द्वारा, और कलियुग में वही भगवान केवल नाम संकीर्तन (नाम जप और भजन) से प्राप्त होते हैं।
पराशर स्मृति
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।
द्वापरे यज्ञमित्यूचुः दानमेकं कलौ युगे ॥
कृतयुग में मोक्ष प्राप्ति को तपस्या को सर्वोच्च माना गया है; त्रेतायुग में ज्ञान को; द्वापरयुग में यज्ञ को; और कलियुग में केवल दान को ही आध्यात्मिक प्रगति का प्रमुख मार्ग माना गया है।
सारांश: JKYog India Online Class- श्रीमद् भागवत कथा [हिन्दी]- 19.05.2025