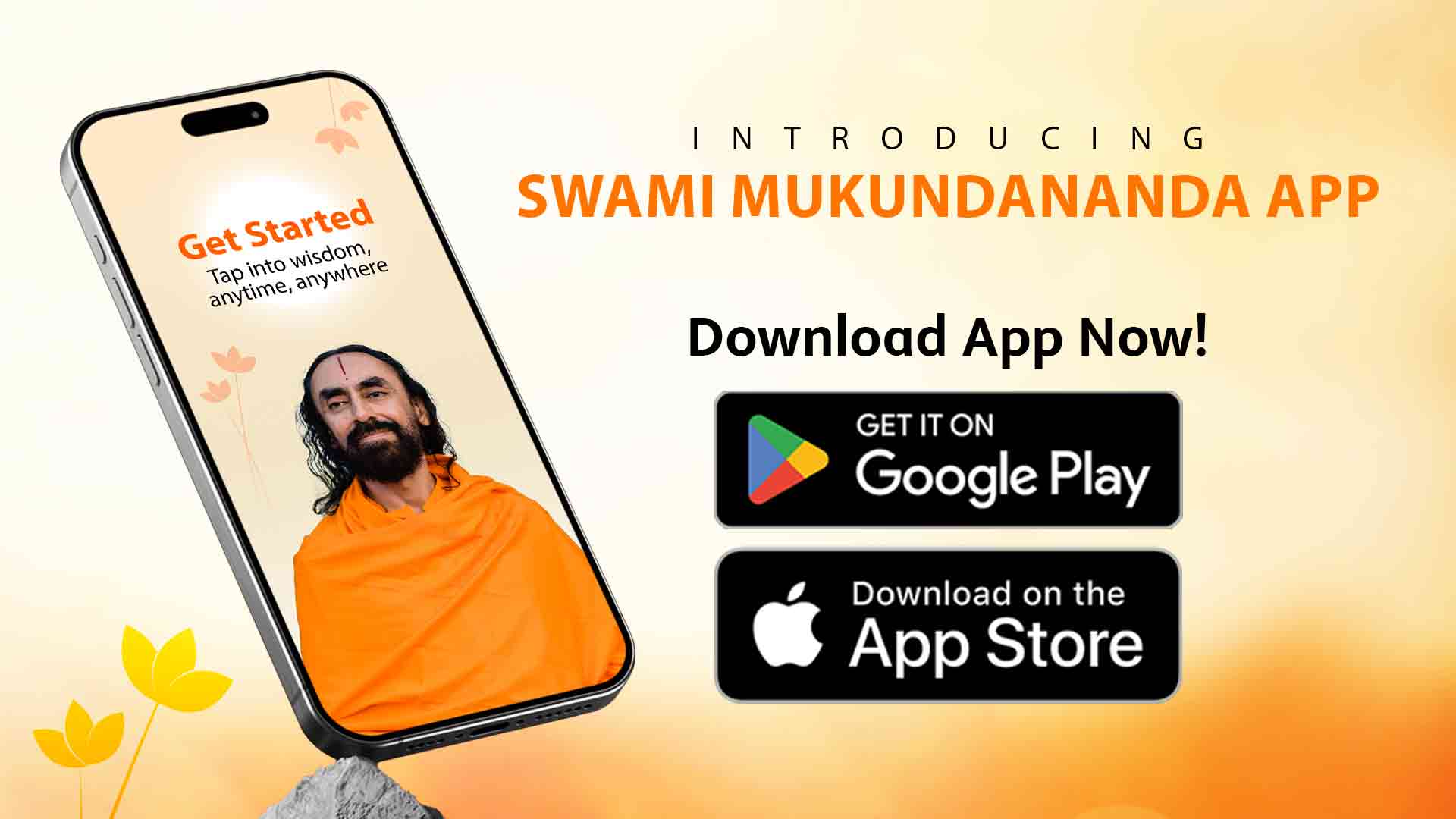श्रीमद्भागवत महापुराण- स्कन्ध: 9 अध्याय: 11-14
श्री शुकदेवजी परीक्षित को श्रीराम की शेष लीलाओं के बारे में बताते हुए कहते हैं की भगवान श्रीराम अपने गुरु वशिष्ठजी को आचार्य बनाकर अनेक यज्ञों का आयोजन करते हैं। यज्ञ में वे स्वयं को ही यजमान बनाकर अपनी सर्वदेवस्वरूप आत्मा का पूजन करते हैं।
उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, अध्वर्यु को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा प्रदान की। शेष भूमि जो बची, वह उन्होंने आचार्य को अर्पित कर दी। इस प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया और अपने पास केवल शरीर पर के वस्त्र और अलंकार ही रखे। इसी प्रकार सीताजी के पास भी केवल मांगलिक आभूषण और वस्त्र मात्र रह गये।
जब ब्राह्मणों ने देखा कि श्रीराम ब्राह्मणों को ही अपना इष्टदेव मानते हैं, तो वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पुनः राम को लौटा दी और उनकी स्तुति करते रहे।
एक दिन, जब भगवान राम रात्रि में नगर की स्थिति जानने के लिए गुप्त रूप से घूम रहे थे, उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को डाँटते हुए कह रहा है, "अरी दुष्टा! तू पराये घर में गई है। स्त्री-लोभी राम भले ही सीता को स्वीकार कर लें, लेकिन मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता।"
जब भगवान राम ने कई लोगों के मुख से ऐसी बातें सुनीं, तो वे लोकापवाद से चिन्तित हो उठे। उन्होंने जनमत का सम्मान करते हुए जानकीजी का परित्याग कर दिया। सीताजी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आकर रहने लगीं। उस समय वे गर्भवती थीं और समय आने पर उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया—लव और कुश। उनके संस्कार वाल्मीकि मुनि ने स्वयं किए।
राम के अनुजों की भी संतानें हुईं—लक्ष्मण के अंगद और चित्रकेतु, भरत के तक्ष और पुष्कल, और शत्रुघ्न के सुबाहु और श्रुतसेन। भरत ने गंधर्वों को पराजित कर उनका धन राम को अर्पित किया। शत्रुघ्न ने लवण नामक राक्षस का वध कर मथुरा नगरी बसाई।
समय आने पर जानकीजी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि मुनि के संरक्षण में सौंप दिया और स्वयं पृथ्वीदेवी की गोद में विलीन हो गईं। यह समाचार सुनकर राम अत्यंत शोकाकुल हुए। यद्यपि वे विवेक और बल में अपार थे, फिर भी जानकीजी के पावन गुणों का स्मरण कर वे व्यथित हो उठे।
इसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया और तेरह हजार वर्षों तक निरंतर अग्निहोत्र करते रहे। अंत समय में अपने भक्तों के हृदयों में अपने चरण स्थापित कर वे अपने परमधाम को प्रस्थान कर गये।
भगवान राम के समान प्रतापशाली कोई नहीं हुआ। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से अवतार लिया और असुरों का नाश कर धर्म की प्रतिष्ठा की। समुद्र पर सेतु बंधन, वानरों की सहायता लेना—यह सब उनकी दिव्य लीला मात्र थी। क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं थी।
उनका यश निर्मल और पवित्र है, जो पापों को नष्ट करता है। उनकी कीर्ति इतनी दूर तक फैली कि आज भी ऋषि-मुनि उनके चरित्र का गान करते हैं और देवता उनके चरणकमलों की सेवा में रहते हैं। मैं भी उन्हीं रघुकुल-शिरोमणि श्रीराम की शरण ग्रहण करता हूँ।
जिन्होंने श्रीराम का साक्षात दर्शन किया, उनके समीप रहे या उनका अनुसरण किया, वे सभी और कोशल के निवासी उसी परमधाम को प्राप्त हुए जहाँ योगी अपने साधन से पहुँचते हैं। जो व्यक्ति उनके पवित्र चरित्र को श्रवण करता है, उसके भीतर सरलता, कोमलता और पवित्रता जैसे दिव्य गुण जाग्रत हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वह अपने कर्मबंधन से मुक्त होकर भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है।
श्रीराम के पुत्र कुश का वंशवृत्तान्त
शुकदेवजी परीक्षित से भगवान राम से आगे के वंश के बारे में कहते हैं – कुश का पुत्र हुआ अतिथि > निषध > नभ > पुण्डरीक > क्षेमधन्वा > देवानीक > अनीह > पारियात्र > बलस्थल > वज्रनाभ (यह सूर्य का अंशावतार था)। वज्रनाभ से खगण > विधृति > हिरण्यनाभ। यह महान योगाचार्य थे। जैमिनि ऋषि का शिष्य थे और याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी उनसे अध्यात्मयोग की शिक्षा प्राप्त की।
हिरण्यनाभ से पुष्य > ध्रुवसन्धि > सुदर्शन > अग्निवर्ण > शीघ्र > मरु > योगसाधना से महान सिद्धि प्राप्त की। वह आज भी कलाप नामक ग्राम में जीवित हैं और कलियुग के अन्त में जब सूर्यवंश नष्ट हो जायेगा, तो वही उसे पुनः स्थापित करेंगे।
मरु से प्रसुश्रुत > सन्धि > अमर्षण > महोस्वान > विश्वसाह > प्रसेनजित > तक्षक > बृहद्बल।यही बृहद्बल कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु (आपके पिता) के हाथों मारे गये थे।
बृहद्बल के बाद के राजे- बृहद्बल से बृहद्रण > उरुक्रिय > वत्सवृद्ध > प्रतिव्योम > भानु > दिवाक (सेनापति) > सहदेव > बृहदश्व > भानुमान > प्रतीकाश्व > सुप्रतीक > मरुदेव > सुनक्षत्र > पुष्कर > अन्तरिक्ष > सुतपा > अमित्रजित > बृहद्राज > बर्हि > कृतंजय > रणंजय > संजय > शाक्य > शुद्धोद > लांगल > प्रसेनजित > क्षुद्रक > रणक > सुरथ > सुमित्र।
सुमित्र ही इस वंश का अन्तिम राजा होगा। उसके समय कलियुग में यह इक्ष्वाकु वंश समाप्त हो जाएगा।
वशिष्ठ के शाप से राजा निमि बनें विदेह
इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मनिष्ठ राजा हुए—निमि। वे अत्यंत सात्विक और भगवान् की भक्ति में रमे रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, “मानव जीवन क्षणभंगुर है, हर श्वास अनिश्चित है। अतः इसे व्यर्थ न गँवाकर, भगवान् की आराधना और यज्ञ में ही समर्पित करना चाहिए।”
ऐसा विचार कर उन्होंने एक महान यज्ञ का संकल्प लिया और उसके आचार्य के लिए महर्षि वशिष्ठजी को बुलवाया।
वशिष्ठजी बोले, “राजन्! इन्द्रदेव ने पहले ही मुझे अपने यज्ञ के लिए नियुक्त कर लिया है। जब उनका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, तब मैं अवश्य आऊँगा। आप कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए।”
राजा निमि के हृदय में एक और ही भावना थी। उन्होंने सोचा, “जीवन का क्या भरोसा? मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। धर्म और भगवान् की सेवा में देरी करना उचित नहीं।” और बिना विलंब किए उन्होंने अन्य महर्षियों को बुलाकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया।
कुछ समय बाद वशिष्ठजी लौटे और देखा कि यज्ञ तो उनके बिना ही प्रारंभ हो गया है। उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, “राजा निमि को अपने ज्ञान पर अहंकार है। अतः इसका शरीर नष्ट हो जाए।”
राजा निमि शांत भाव से उत्तर देते हैं, “गुरुवर! आपने भी इन्द्र के लोभ में आकर धर्म की उपेक्षा की है, इसलिए आपका शरीर भी नष्ट हो।”
इस प्रकार दोनों ने देह त्याग दी। आत्मज्ञान में निपुण राजा निमि परम शांति को प्राप्त हुए और वशिष्ठजी बाद में मित्रावरुण के यज्ञ से उर्वशी के गर्भ में पुनः अवतरित हुए।
ऋषियों ने राजा निमि के शरीर को सुरक्षित रखा और यज्ञ पूरा होने के बाद जब देवता प्रकट हुए, तो उनसे प्रार्थना की, “हे देवगण! यदि आप प्रसन्न हों तो हमारे राजा को पुनः जीवन दीजिए।”
देवताओं ने कहा, “सो होगा।”
परन्तु निमि बोले, “मैं अब शरीर नहीं चाहता। यह शरीर तो दुःख, शोक और भय का निवास है। जैसे मछली हर जगह मृत्यु से घिरी रहती है, वैसे ही जीव देह के साथ हर पल मृत्यु से घिरा है। मैं अब मुक्त होकर केवल भगवान् का स्मरण करना चाहता हूँ।”
देवताओं ने आशीर्वाद दिया, “तथास्तु! अब राजा निमि शरीर धारण किए बिना ही सबके नेत्रों में निवास करेंगे। पलक झपकने के क्षण मात्र में जो आभास होता है, वही निमि का अस्तित्व है।”
इसी कारण उस क्षणभर को “निमेष” कहा जाने लगा। एक निमेष वही समय है, जितना समय मनुष्य को आँख झपकने में लगता है।
किन्तु ऋषियों को चिंता हुई, “यदि राजा नहीं रहे तो प्रजा का क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी।” इसलिए उन्होंने राजा निमि के सुरक्षित शरीर का मंथन किया और उससे एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। ऋषियों ने उसका नाम रखा जनक। क्योंकि वह विदेह निमि से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसे वैदेह भी कहा गया। और चूँकि वह शरीर के मंथन से उत्पन्न हुआ था, उसका नाम मिथिल पड़ा। उसी जनक ने आगे चलकर मिथिला नगरी बसाई।
राजा जनक से आगे का वंश-वृत्त
जनक से उदावस > नन्दिवर्धन > सुकेतु > देवरात > बृहद्रथ > महावीर्य > सुधृति > धृष्टकेतु > हर्यश्व > मरु > प्रतीपक > कृतिरथ > देवमीढ > विश्रुत > महाधुति > कृतिरात > महारोमा > स्वर्णरोमा > ह्रस्वरोमा।
ह्रस्वरोमा के पुत्र सीरध्वज थे। जब वे यज्ञ हेतु धरती जोत रहे थे, तो उनके हल की नोक (फाल) से सीता जी प्रकट हुईं। सीरध्वज के पुत्र कुशध्वज > धर्मध्वज से दो पुत्र हुए – कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज से केशिध्वज और मितध्वज से खाण्डिक्य। केशिध्वज आत्मविद्या के ज्ञाता थे, और खाण्डिक्य कर्मकाण्ड में निपुण। खाण्डिक्य उनसे भयभीत होकर भाग गये।
केशिध्वज से भानुमान > शतद्युम्न > शुचि > सनद्वाज > ऊर्ध्वकेतु > अज > पुरुजित > अरिष्टनेमि > श्रुतायु > सुपार्श्वक > चित्ररथ > क्षेमधि > समरथ > सत्यरथ > उपगुरु > उपगुप्त (अग्नि का अंश) > वस्वनन्त > युयुध > सुभाषण > श्रुत > जय > विजय > ऋत > शुनक > वीतहव्य > धृति > बहुलाश्व > कृति > महावशी।
चंद्र ने किया तारा का अपहरण और हुआ बुध का जन्म
श्रीशुकदेवजी परीक्षित को चन्द्रमा के वंश की कथा सुनते हैं। यह वंश बहुत महान है और इसमें पुरूरवा जैसे तेजस्वी राजाओं का जन्म हुआ। ब्रह्माजी के पुत्र अत्रि हुए। अत्रि इतने गुणवान थे कि उन्हें देखकर लोग स्वयं ब्रह्माजी समझ बैठते थे। इन्हीं अत्रि ऋषि की आंखों से अमृतमय तेज निकलकर चन्द्रमा प्रकट हुए। ब्रह्माजी ने चन्द्रमा को ब्राह्मणों, औषधियों और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया।
धीरे-धीरे चन्द्रमा को शक्ति और वैभव प्राप्त हुआ। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय पाई और राजसूय यज्ञ किया। इस सफलता से उनमें अभिमान आ गया। गर्व में चूर होकर उन्होंने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया।
बृहस्पति ने बार-बार विनती की, "हे चन्द्र! मेरी पत्नी को लौटा दो।"
परंतु अहंकार से अंधे चन्द्रमा ने बात नहीं मानी। इससे देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। शुक्राचार्य असुरों के साथ खड़े हो गये और महादेवजी ने अपने गुरु बृहस्पति का पक्ष लिया। देवताओं और असुरों का ऐसा घमासान हुआ मानो प्रलय ही हो रही हो।
तभी अंगिरा ऋषि ब्रह्माजी के पास पहुंचे और युद्ध रोकने की प्रार्थना की। ब्रह्माजी ने चन्द्रमा को डांटा और तारा को उसके पति बृहस्पति के पास लौटा दिया।
लेकिन तारा गर्भवती थी। बृहस्पति ने क्रोध से कहा, “यह बच्चा मेरा नहीं है, इसे त्याग दो।”
लज्जित तारा ने स्वर्ण के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक को देखकर चन्द्रमा और बृहस्पति दोनों ही मोहित हो गये और कहने लगे, “यह मेरा है!”
सभी ने तारा से पूछा, “सच बताओ, यह किसका पुत्र है?”
लज्जा से चुप रहने पर बालक ने ही क्रोधित होकर कहा, “माँ! झूठ मत बोलो। सच बताओ, मैं किसका पुत्र हूँ?”
अंत में ब्रह्माजी ने तारा को समझाया और तब उसने कहा, “यह चन्द्रमा का पुत्र है।”
ब्रह्माजी ने उसका नाम रखा बुध। बुध से पुरूरवा का जन्म हुआ।
पुरूरवा और उर्वशी की कथा
एक बार इन्द्र की सभा में नारदजी पुरूरवा की प्रशंसा कर रहे थे। वे कह रहे थे, “पुरूरवा जितने वीर हैं उतने ही रूपवान और उदार भी हैं।” यह सुनकर अप्सरा उर्वशी का हृदय डोल उठा। वैसे भी मित्रावरुण के शाप से उसे पृथ्वी पर आना ही था।
उर्वशी जब पुरूरवा के सामने आयी तो राजा की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने कहा, “सुन्दरी! तुम्हारा स्वागत है। आओ, बैठो। मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? आओ, मेरे साथ विहार करो और हमारा यह संग अनन्त काल तक चलता रहे।”
उर्वशी ने मुस्कुराकर कहा, “राजन्! आपका रूप देखकर कौन स्त्री मोहित नहीं होगी? मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। पहला, आप मेरे सौंपे हुए दो मेमनों की रक्षा करेंगे। दूसरा, मैं केवल घी खाऊँगी। और तीसरा, मैथुन के अतिरिक्त किसी भी समय मैं आपको वस्त्रहीन अवस्था में नहीं देखूँगी।”
राजा ने तुरन्त हामी भर दी।
अब दोनों साथ-साथ नन्दनवन और चैत्ररथ जैसे उपवनों में घूमते, हँसते और प्रेम करते। उर्वशी के शरीर से कमल की सुगन्ध आती थी, जिससे राजा मदहोश रहते।
परन्तु इन्द्र उर्वशी के बिना अधीर हो उठे। उन्होंने गन्धर्वों को भेजा कि किसी तरह उर्वशी को वापस लाओ। गन्धर्व आधी रात को आये और वे दोनों मेमने चुरा ले गये।
जब उर्वशी ने अपने प्रिय मेमनों की आवाज सुनी तो वह तिलमिला उठी और राजा पर व्यंग्य बाण चलाये, “देखो, यह कैसे वीर हैं! मेरे मेमनों को भी न बचा सके। दिन में तो खुद को बड़ा वीर मानते हैं, रात में औरतों की तरह सोये रहते हैं।”
इन कटु वचनों ने पुरूरवा का हृदय छलनी कर दिया। वे तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में दौड़े और मेमनों को बचा लाए। लेकिन उसी प्रकाश में उर्वशी ने उन्हें नग्न देख लिया और उसी क्षण वचन के अनुसार उन्हें छोड़कर चली गयी।
पुरूरवा उर्वशी के वियोग में पागल हो गये। वे जगह-जगह उसे खोजते फिरते। एक बार सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी सखियों को देखा। वे विनती करने लगे, “प्रिये! मुझे मत छोड़ो। क्षणभर ठहर जाओ। तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है।”
उर्वशी ने ठंडी सांस लेकर कहा, “राजन्! आप पुरुष हैं, इस तरह दुखी होकर मत मरिये। जान लीजिए, स्त्रियाँ किसी की स्थायी मित्र नहीं होतीं। उनका स्वभाव चंचल और निर्दयी होता है। वे ज़रा-सी बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े-बड़े काम कर बैठती हैं। इसलिए आप धीरज रखिए। आप तो राजा हैं, आपको घबराना नहीं चाहिए। साल में एक बार, एक रात मैं आपके साथ रहूँगी और तब आपको संतान भी मिलेगी।”
पुरूरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है। वे अपनी राजधानी लौट गये। एक वर्ष बाद जब वे फिर उससे मिलने आये तो वह पहले ही एक वीर पुत्र की माँ बन चुकी थी।
उर्वशी से मिलकर पुरूरवा को बहुत सुख मिला। वे एक रात उसके साथ रहे। सुबह जब विदा का समय आया तो पुरूरवा विरह के दुख से बहुत उदास हो गये। तब उर्वशी ने कहा, “आप गन्धर्वों की स्तुति कीजिए। अगर वे चाहें तो मुझे आपको सौंप सकते हैं।”
पुरूरवा ने गन्धर्वों की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर गन्धर्वों ने उन्हें अग्निस्थाली (अग्नि स्थापित करने का पात्र) दी। पुरूरवा समझ बैठे कि यही उर्वशी है। उन्होंने उस अग्निस्थाली को सीने से लगा लिया और वन-वन भटकते रहे।
जब होश आया, तब उन्होंने स्थाली को वहीं वन में छोड़ दिया और अपने महल लौट आये। रात को वे उर्वशी का ही ध्यान करते रहते।
समय बीता और त्रेतायुग का प्रारम्भ हुआ। तब पुरूरवा के हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए।
वे उस स्थान पर गये जहाँ उन्होंने अग्निस्थाली छोड़ी थी। वहाँ एक पीपल का पेड़ उग आया था। उन्होंने उस वृक्ष की लकड़ी से दो अरणियाँ (मन्थन करने वाले लकड़ी के टुकड़े) बनायीं। उन्होंने कल्पना की कि नीचे की अरणि उर्वशी है, ऊपर की अरणि वे स्वयं हैं और बीच का टुकड़ा उनका पुत्र है।
मन्त्रों के साथ मन्थन करने से अग्नि प्रकट हुई, जिसे ‘जातवेदा’ कहा गया। पुरूरवा ने अग्नि को पुत्र के समान माना और उसे तीन रूपों में बाँट दिया – आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि। फिर उर्वशी की इच्छा पूरी करने के लिए, उन्हीं तीन अग्नियों के द्वारा पुरूरवा ने यज्ञपति भगवान श्रीहरि की पूजा की।
श्री शुकदेवजी परीक्षित को कहते हैं की सत्ययुग में तो केवल एक ही वेद था – प्रणव (ॐकार)। सभी शास्त्र उसी में समाए हुए थे। देवता भी केवल एक ही थे – नारायण। अग्नि भी एक ही था और समाज में केवल एक ही वर्ण था – ‘हंस’। परंतु त्रेतायुग की शुरुआत से वेद तीन हुए और अग्नि भी तीन रूपों में प्रकट हुई। पुरूरवा ने अग्नि को संतान रूप में स्वीकार किया और अंत में गन्धर्वलोक की प्राप्ति की।
सारांश: JKYog India Online Class- श्रीमद् भागवत कथा [हिन्दी]- 25.08.2025