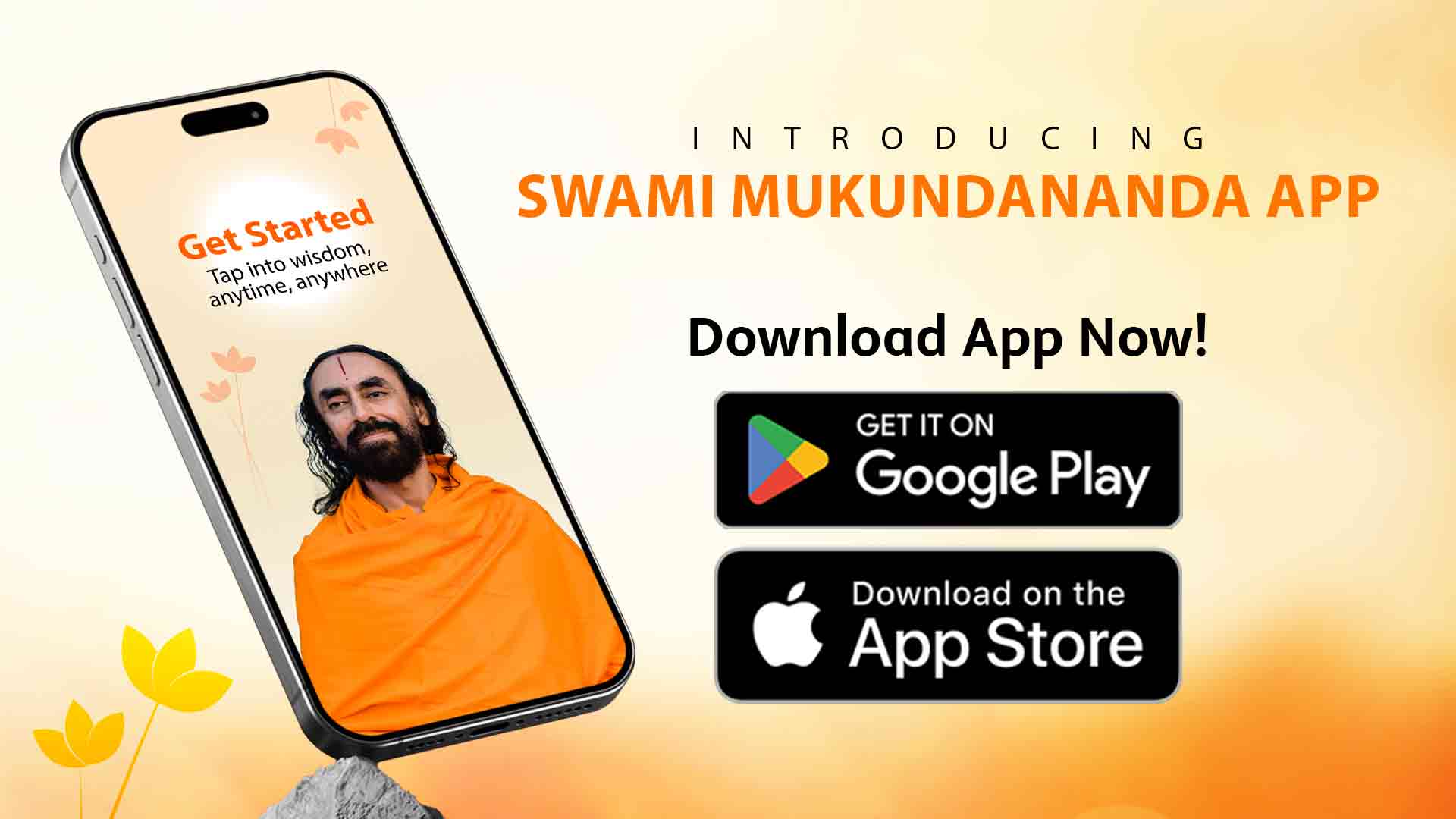श्रीमद्भागवत महापुराण- स्कन्ध: 7 अध्याय: 4-5
ब्रह्माजीसे अत्यन्त दुर्लभ वरदान पाकर हिरण्यकशिपु का शरीर तेजस्वी और बलवान हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु को याद करके भगवान से द्वेष करने लगा और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सभी प्राणियों को अपने अधीन कर लिया—देवता, मनु, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस आदि सभी। उसने इन्द्र का महल छीन लिया और स्वर्ग में ही निवास करने लगा।
उसका महल ऐश्वर्य से भरपूर था—रत्नों से जड़ी दीवारें, सुंदर अप्सराएँ, विलासिता का हर साधन। वह सब देवताओं का अधिपति बन बैठा और इतना शक्तिशाली हो गया कि बड़े-बड़े यज्ञों की आहुतियाँ भी स्वयं ले लेता। सारे देवता भय के कारण उसकी सेवा में लगे रहते। उसका शासन सातों द्वीपों तक था। भूमि बिना जोते अनाज देती, समुद्र रत्न पहुंचाते, पर्वत उसके खेल का स्थान बनते और वृक्ष सदा फलते-फूलते। फिर भी उसे संतोष नहीं था—क्योंकि वह इन्द्रिय-सुखों का दास बन गया था।
नारदजी बताते हैं, “युधिष्ठिर, इतना सब होते हुए भी वह वही हिरण्यकशिपु है, जो पूर्वजन्म में भगवान का पार्षद था और सनकादिक मुनियों के शाप से असुर बना। अब वह घमंड और अहंकार में डूबकर धर्म की सीमाओं का उल्लंघन कर रहा था। समय बीतता जा रहा था, पर वह मोह में फंसा हुआ था।”
हिरण्यकशिपु के अत्याचार से सभी लोक और लोकपाल भयभीत हो गये। जब कहीं भी आश्रय नहीं मिला, तब उन्होंने अन्ततः भगवान श्रीहरि की शरण ली। उन्होंने मन ही मन भगवान के उस परम धाम को प्रणाम किया, जहाँ पहुँचकर महात्मा सदा के लिए शांत हो जाते हैं और लौटते नहीं। फिर उन्होंने अपनी इन्द्रियाँ संयमित कर लीं, मन को एकाग्र किया, और भोजन, निद्रा का त्याग कर शुद्ध हृदय से भगवान की आराधना करने लगे।
तब एक दिन उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी—बिलकुल मेघ के समान गंभीर और दिशाओं को गुंजा देने वाली, “हे श्रेष्ठ देवगण! भय मत करो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। इस पापी दैत्य की दुष्टता मुझे पहले से ही ज्ञात है। सही समय आने पर मैं इसे समाप्त कर दूंगा। जो भी प्राणी देवता, वेद, धर्म, ब्राह्मण, गाय, साधु और मुझसे द्वेष करता है, उसका शीघ्र ही नाश होता है। जब यह अपने निष्पाप और भक्त पुत्र प्रह्लाद से वैर करेगा, तब— अपने वरदानों के बल पर भी—यह मुझसे नहीं बच पाएगा। मैं स्वयं इसे मारूंगा।” भगवान की यह वाणी सुनकर देवता आश्वस्त हो गये। उन्हें ऐसा लगा मानो हिरण्यकशिपु अभी मारा गया हो। वे शांत और निश्चिंत होकर लौट आये।
प्रह्लादजी के गुणों का वर्णन
नारदजी आगे कहते हैं की हिरण्यकशिपु के चार पुत्रों में सबसे छोटे प्रह्लाद थे, लेकिन गुणों में सबसे श्रेष्ठ। वे संतों के सेवक, ब्राह्मणों के भक्त, सौम्य स्वभाव के, सत्यनिष्ठ और इन्द्रियों के विजेता थे। प्रह्लाद सब प्राणियों में समानता देखते थे—बड़ों के चरणों में सेवक बनकर झुकते, गरीबों पर पिता जैसा स्नेह रखते, समकक्षों से भाई जैसा व्यवहार करते और गुरुओं में उन्हें भगवान का भाव दिखता। विद्या, धन, कुल और सौंदर्य से संपन्न होने के बावजूद उनमें कभी अहंकार नहीं आया। बड़े से बड़े संकट भी उन्हें विचलित नहीं कर पाते। उन्होंने संसार और परलोक के विषयों को जानकर भी उन्हें असार समझा, इसलिए किसी भी वस्तु की इच्छा उनके मन में नहीं थी। इन्द्रियाँ, मन, शरीर और प्राण— उनके पूर्ण वश में थे। उनमें जन्म से असुर कुल का हिस्सा होने पर भी कोई आसुरी गुण नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रह्लाद के भी।
देवता भले ही उनके शत्रु हों, लेकिन भक्तों की सभा में वे प्रह्लाद का नाम लेकर दूसरे भक्तों की भी प्रशंसा करते हैं। इसलिए युधिष्ठिर! आप जैसे अजातशत्रु भगवद्भक्त के लिए प्रह्लाद के प्रति श्रद्धा रखना तो स्वाभाविक ही है। उनकी महिमाका वर्णन करनेके लिये अगणित गुणोंके कहने-सुननेकी आवश्यकता नहीं। केवल एक ही गुण- श्रीकृष्णके चरणोंमें स्वाभाविक, जन्मजात प्रेम उनकी महिमाको प्रकट करनेके लिये पर्याप्त है।
- प्रह्लादजी बचपन से ही खेल-कूद छोड़कर भगवान श्रीकृष्ण के ध्यान में लीन हो जाते थे।
- श्रीकृष्ण के अनुग्रह से उनका हृदय ऐसा खिंच गया था कि संसार की सुध-बुध खो बैठते थे। उन्हें अनुभव होता था कि भगवान उन्हें गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं।
- चलते-फिरते, खाते-पीते, बात करते समय भी उनका मन निरंतर भगवान में लगा रहता था।
- प्रेम के विविध भाव: भगवान को ओझल मानकर रो पड़ते, उनके दर्शन से आनंद में हँस पड़ते, ध्यान में लीन होकर गाने लगते, कभी बेसुरा चिल्ला पड़ते, कभी लोक-लज्जा भूलकर प्रेम में नाचने लगते।
- भगवान की लीलाओं में इतना तन्मय हो जाते कि उनकी नकल करने लगते। श्रीकृष्ण के कोमल स्पर्श का अनुभव कर चुपचाप पुलकित हो जाते; नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते।
- यह दिव्य भक्ति उन्हें अकिंचन भगवत्प्रेमी महात्माओं की संगति से प्राप्त हुई थी। स्वयं परमानंद में रहते हुए, वे कुसंग से दुखी जीवों को भी अपने प्रेम से शांति देते थे।
नारदजी आगे कहते हैं कि प्रह्लाद भगवान्के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान् और ऊँची कोटिके महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु पुत्रको भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करनेकी चेष्टा करने लगा । युधिष्ठिरने पूछा, “नारदजी! हिरण्यकशिपुने पिता होकर भी ऐसे शुद्धहृदय महात्मा पुत्रसे द्रोह क्यों किया। पिता तो स्वभावसे ही अपने पत्रोंसे प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उलटा काम करता है, तो वे उसे शिक्षा देनेके लिये ही डाँटते हैं, शत्रुकी तरह वैर-विरोध तो नहीं करते।”
इसपर नारदजी युधिष्ठिर से कहते हैं कि दैत्यगण ने शुक्राचार्यजी को अपना गुरु और पुरोहित बना रखा था। उनके दो पुत्र – शण्ड और अमर्क – हिरण्यकशिपु के आदेश पर प्रह्लाद और अन्य दैत्यबालकों को राजनीति और अर्थनीति सिखाते थे। प्रह्लादजी गुरु का पाठ सुन लेते और दोहरा भी देते, लेकिन मन से उसे स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि वह ‘मैं’ और ‘मेरा’ के अहंकार से प्रेरित था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने स्नेहपूर्वक प्रह्लाद को गोद में बैठाकर पूछा – “बेटा! तुम्हें सबसे प्रिय बात क्या लगती है?”
प्रह्लाद ने निर्भीक होकर उत्तर दिया – “पिताजी! यह संसार ‘मैं’ और ‘मेरा’ के मोह में फँसकर दुखी रहता है। इसलिए मैं यही उचित समझता हूँ कि ऐसे लोग घर रूपी अंधे कूएं को छोड़कर वन में जाकर श्रीहरि की शरण लें।”
यह सुनकर हिरण्यकशिपु पहले तो हँस पड़ा और सोचा कि शायद कोई विष्णुभक्त ब्राह्मण भेष बदलकर गुरु के घर में घुसा है और बालक की बुद्धि बिगाड़ रहा है। उसने आदेश दिया कि अब प्रह्लाद की निगरानी और कड़ी की जाए ताकि उसकी सोच न भटके।
जब प्रह्लाद को फिर से शण्ड-अमर्क के पास भेजा गया, तो वे बड़े प्रेम से और फुसलाकर बोले – "बेटा प्रह्लाद! सच्च-सच्च बताओ, तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों हो गई? क्या किसीने तुम्हें बहकाया है, या यह तुम्हारे मन की बात है?"
प्रह्लाद ने उत्तर दिया – "जिनकी बुद्धि मोह में फँसी होती है, वही ‘मैं’ और ‘मेरा’, ‘अपना’ और ‘पराया’ जैसे झूठे भेद करते हैं। पर यह सब भगवान की माया है। जब भगवान् कृपा करते हैं, तभी यह भ्रम मिटता है। भगवान ही सबके आत्मा हैं, लेकिन अज्ञानी लोग भेदभाव करते हैं। जैसे लोहे को चुम्बक खींच लेता है, वैसे ही मेरे चित्त को भगवान श्रीहरि अपनी कृपा से खींच लेते हैं।"
परमज्ञानी प्रह्लाद अपने गुरुजीसे इतना कहकर चुप हो गये। लेकिन वे पुरोहित बेचारे राजाके सेवक एवं पराधीन थे। वे डर गये। उन्होंने क्रोधसे प्रह्लादको झिड़क दिया और कहा- "यह बालक तो हमारे कुल की मर्यादा पर दाग लगा रहा है। इसे अब डांट-डपट से नहीं, दण्ड से ठीक करना होगा।" उन्होंने उसे ‘दैत्यकुल का काँटा’ और विष्णुभक्त कहकर अपमानित किया, और फिर उसे अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। समय बीता। जब उन्होंने समझा कि प्रह्लाद ने सारी नीतियाँ जान ली हैं तब वे उसे उसकी माता के पास ले गये। माताजी ने उसे स्नेह से सजाया-संवारा और फिर हिरण्यकशिपु के पास ले गयीं। प्रह्लाद अपने पिताके चरणोंमें लोट गये। हिरण्यकशिपुने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथोंसे उठाकर – बहुत देरतक गलेसे लगाये रखा और कहा, "चिरंजीव बेटा प्रह्लाद! इतने दिनोंमें तुमने गुरुजीसे जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमेंसे कोई अच्छी-सी बात हमें सुनाओ।"
श्रीप्रह्राद उवाच।
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ।
इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा। क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम् ।
प्रह्लादजीने कहा-पिताजी! विष्णुभगवान्की भक्तिके नौ भेद हैं-भगवान्के गुणलीला-नाम आदिका श्रवण, उन्हींका कीर्तन, उनके रूप-नाम आदिका स्मरण, उनके चरणोंकी सेवा, पूजा-अर्चा, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान्के प्रति समर्पणके भावसे यह नौ प्रकारकी भक्ति की जाय, तो मैं उसीको उत्तम अध्ययन समझता हूँ। (भागवत 7.5.23-24)
नवधा भक्ति कौन से हैं?
- श्रवणम् – भगवान की कथा, नाम, गुण, लीला आदि को सुनना।
- कीर्तनम् – उनका नाम, गुण और लीला का कीर्तन करना।
- स्मरणम् – मन, बुद्धि से निरंतर उनका स्मरण करना।
- पादसेवनम् – उनके चरणों की सेवा करना।
- अर्चनम् – पूजन द्वारा भगवान की उपासना करना।
- वन्दनम् – उन्हें दण्डवत प्रणाम करना।
- दास्यम् – स्वयं को उनका दास मानकर सेवा करना।
- सख्यम् – भगवान को मित्रभाव से देखना और व्यवहार करना।
- आत्मनिवेदनम् – अपनी आत्मा, जीवन और सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना।
प्रह्लादकी यह बात सुनते ही क्रोधके मारे हिरण्यकशिपके ओठ फडकने लगे। उसने गुरुपुत्रसे कहा,"रे नीच ब्राह्मण! यह तेरी कैसी करतूत है; दुर्बुद्धि! तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चेको कैसी निस्सार शिक्षा दे दी? अवश्य ही तू हमारे शत्रुओंके आश्रित है। संसारमें ऐसे दुष्टोंकी कमी नहीं है, जो मित्रका बाना धारणकर छिप-छिपे शत्रुका काम करते हैं। परन्तु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है, जैसे छिपकर पाप करनेवालोंका पाप समयपर रोगके रूपमें प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है।"
गुरुपुत्रने कहा की आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है, वह मेरे या और किसीके बहकानेसे नहीं कह रहा है। यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शान्त कीजिये। व्यर्थमें हमें दोष न लगाइये। जब गुरुजीने ऐसा उत्तर दिया, तब हिरण्यकशिपुने फिर प्रह्लादसे पूछा, "क्यों रे! यदि तुझे ऐसी अहित करनेवाली खोटी बुद्धि गुरुमुखसे नहीं मिली तो बता, कहाँसे प्राप्त हुई?"
प्रह्लादजी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, "पिताजी! यह बुद्धि गुरुजन या किसी सांसारिक व्यक्ति से नहीं मिलती। जो लोग इन्द्रियों के वश में होकर संसाररूपी नरक में बार-बार गिरते हैं, वे केवल भोगों के पीछे भागते हैं। उनकी बुद्धि कभी भी भगवान श्रीकृष्ण में नहीं लगती। सच्चा कल्याण तो उन्हीं को मिलता है जो भगवद्भक्त महात्माओं की संगति करते हैं। वही लोग भगवान के चरणकमलों का स्पर्श कर पाते हैं, जिससे जन्म और मृत्यु के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं।"
प्रह्लाद की यह सत्य और गूढ़ बातें सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से अंधा हो गया। उसने प्रह्लाद को गोद से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और उसने दैत्य सैनिकों से कहा, "इस विष्णु भक्त बालक को अभी इसी समय मार डालो! जिस विष्णु ने मेरे भाई (हिरण्याक्ष) को मारा, उसी के चरणों की पूजा करने वाला यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। हो सकता है, यह स्वयं विष्णु ही किसी रूप में मुझ तक पहुँच गया हो। पाँच वर्ष की उम्र में जिसने माता-पिता को त्याग दिया, वह दयालु नहीं – कृतघ्न (अहितकारी) है। यदि कोई अपना पुत्र भी शत्रु के समान व्यवहार करे, तो उसे शरीर के रोग जैसे काट देना चाहिए ताकि बाकी शरीर सुरक्षित रह सके। इस बालक को किसी भी समय—सोते, खाते या चलते—मार डालो। यह पुत्र भेष में शत्रु है।"
सारांश: JKYog India Online Class- श्रीमद् भागवत कथा [हिन्दी]- 05.05.2025