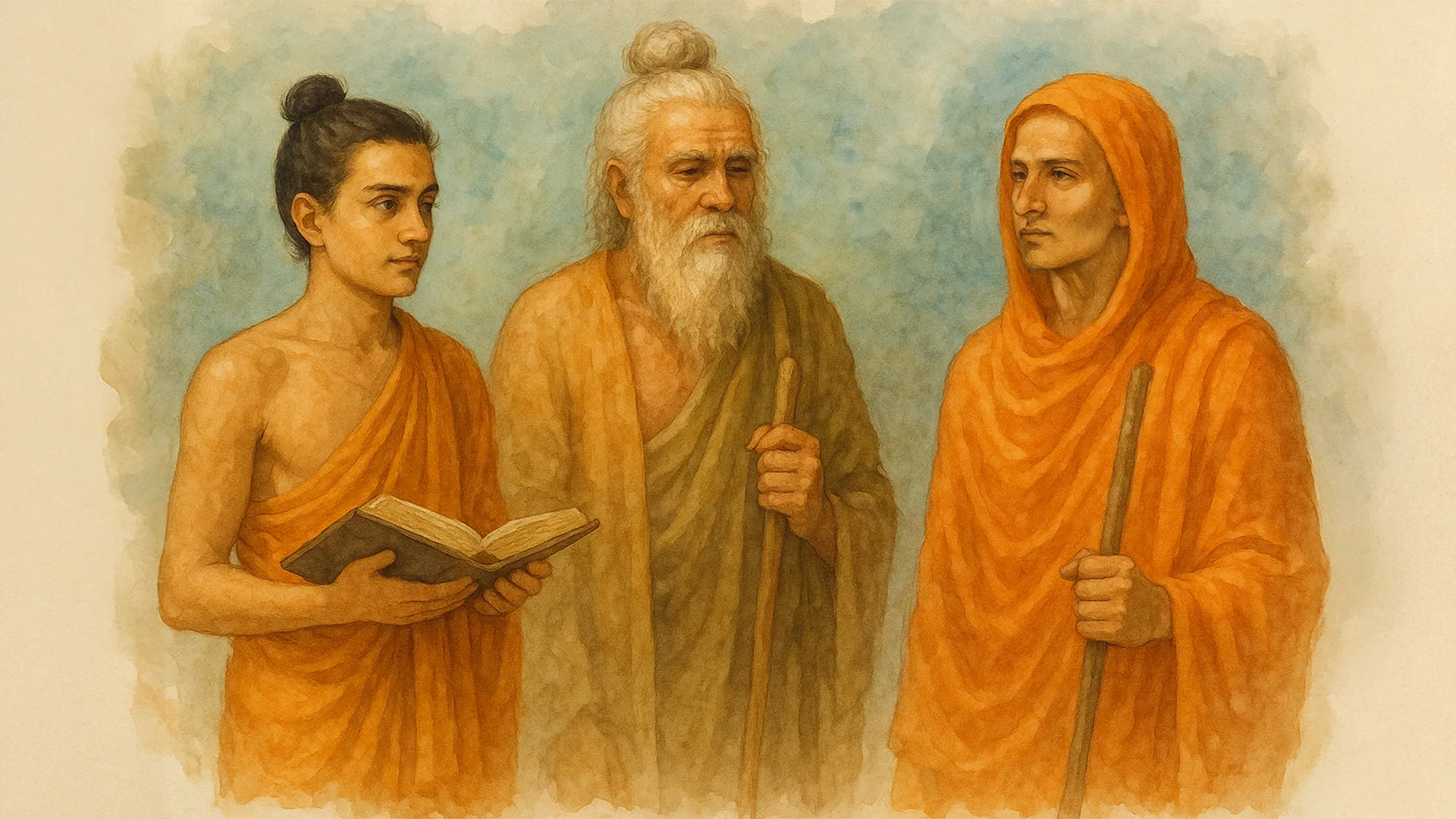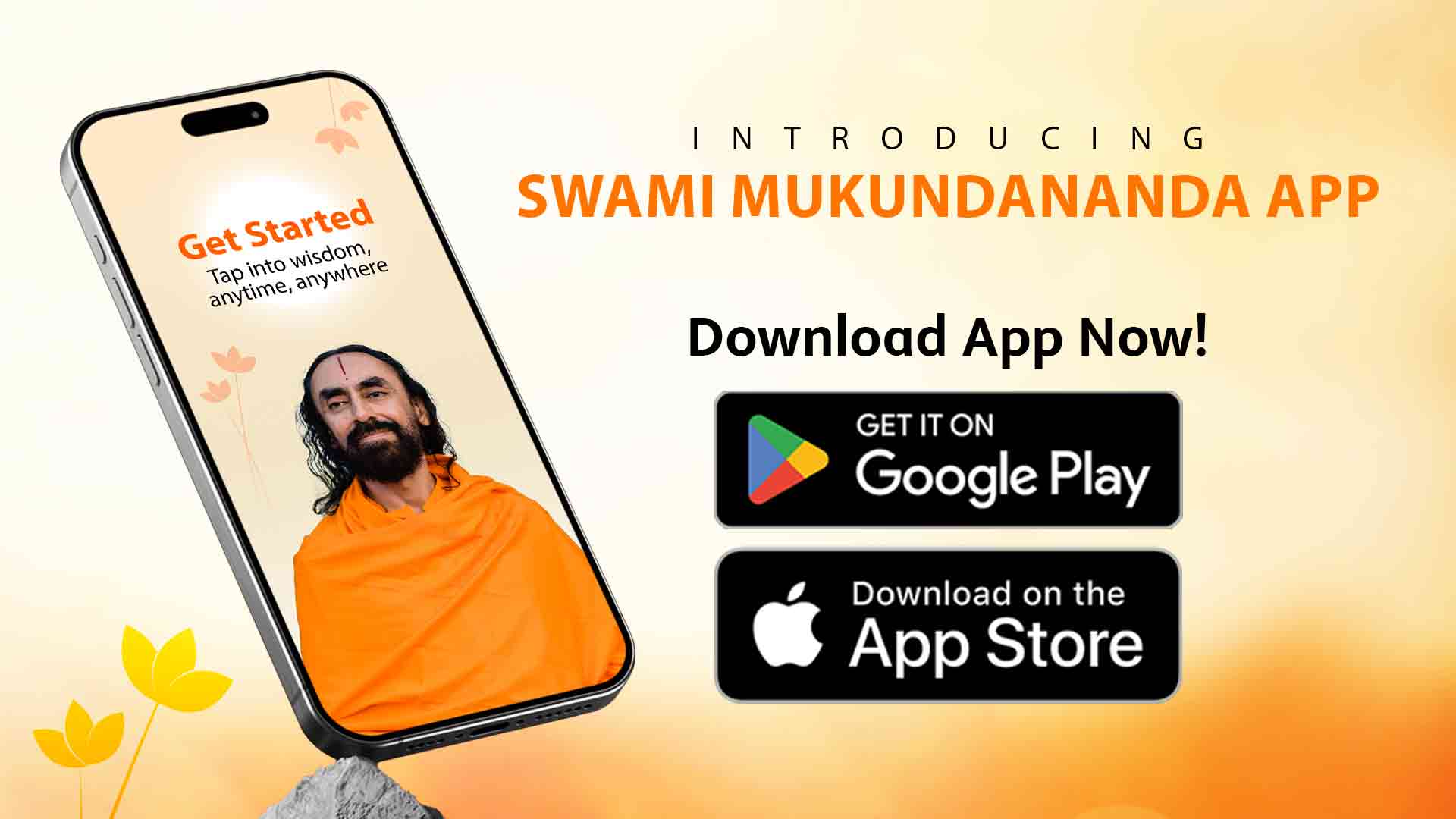श्रीमद्भागवत महापुराण- स्कन्ध: 7 अध्याय: 12-13
वर्ण के विषय में बताने के पश्चात नारदजी युधिष्ठिर को विभिन्न आश्रमों के बारे में उपदेश देते हैं। सबसे पहले वे ब्रह्मचारी आश्रम के नियम बताते हैं। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह अपनी इन्द्रियों को वश में रखे, स्वयं को दास के समान विनम्र माने और गुरुदेव के चरणों में गहरी भक्ति रखे। वह गुरु के कार्यों में समर्पण भाव से सहायता करे। उसे प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा मौन रहकर एकाग्रता से गायत्री मंत्र का जप करते हुए संध्या-वंदन करना चाहिए।
उसे शास्त्रानुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दण्ड, कमण्डलु, यज्ञोपवीत और कुश आदि धारण करना चाहिए। तेल, सुरमा, उबटन, स्त्रियों के चित्र, मांस, मदिरा, पुष्पमालाएं, इत्र, चंदन और आभूषणों का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचारी को सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांगकर लानी चाहिए और उसे गुरु को समर्पित कर देना चाहिए, फिर यदि गुरु आज्ञा दें तभी भोजन करे, अन्यथा उपवास करे।
वह अपने शील की रक्षा करे, संयमित आहार ले, कार्यों को दक्षता से संपन्न करे, श्रद्धा रखे और इन्द्रियों पर नियंत्रण बनाए रखे। स्त्रियों से केवल आवश्यकता भर ही व्यवहार करे, क्योंकि इन्द्रियाँ अत्यंत बलवान होती हैं और साधना में भी विघ्न डाल सकती हैं। जब तक आत्मसाक्षात्कार नहीं होता, तब तक 'मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है' का द्वैत बना रहता है और भोग की भावना उत्पन्न हो सकती है। ये सभी नियम ब्रह्मचारी, गृहस्थ और संन्यासी सभी के लिए उपयोगी हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर सेवा करना वैकल्पिक हो सकता है।
इस प्रकार गुरुकुल में रहकर ब्राह्मण को वेद, वेदांग और उपनिषदों का अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुँहमांगी दक्षिणा दे और उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे।
अब नारदजी युधिष्ठिर को ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताते हैं, जिनका पालन करने से वानप्रस्थी को महर्लोक जैसे ऋषियों के दिव्य लोक की सहज प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ को जोती हुई भूमि पर उगाए गए अन्न या असमय पके अन्न नहीं खाने चाहिये। अग्नि से पका हुआ या कच्चा अन्न भी न खाए। केवल सूर्य की गर्मी से पके कंद, मूल, फल आदि का सेवन करे। वह वन में स्वयं उगने वाले धान्यों से नियमित और विशेष हवन करता रहे, और जैसे ही नए फल, फूल आदि मिलने लगें, पुराने संग्रहित अन्न को त्याग दे। अग्निहोत्र की रक्षा के लिए वह झोंपड़ी या गुफा का आश्रय ले सकता है, परंतु शीत, गर्मी, वर्षा आदि प्राकृतिक स्थितियों को स्वयं सहन करे। सिर पर जटा रखे, बाल-नख-रोम न कटवाए और शरीर पर लगी मैल को भी वैसे ही बनाए रखे। साथ में कमंडलु, मृगचर्म, दण्ड, वल्कल वस्त्र और यज्ञ सामग्री रखे।
पुरुष को अपनी क्षमता अनुसार 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए, किंतु तपस्या इतनी भी न हो कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। जब शरीर रोगग्रस्त हो जाए या बुढ़ापे में वेदांत का मनन भी न हो सके, तब वह अनशन आदि व्रतों द्वारा जीवन का परित्याग कर सकता है। अनशन से पूर्व अग्नियों को आत्मा में लीन करे और ‘मैं’ व ‘मेरा’ का त्याग कर शरीर को उसके मूल तत्वों में विलीन करे। इन्द्रियों और शरीर के अंगों को उनके कारणभूत तत्त्वों में क्रमशः लीन करे—जैसे प्राण वायु में, गर्मी अग्नि में, तरल तत्व जल में, हड्डियाँ पृथ्वी में और छिद्राकाश आकाश में। इस प्रकार अंत में जो शुद्ध चैतन्य आत्मा शेष बचती है, वही आत्मस्वरूप है—'वह मैं हूँ'—इस भाव से अद्वैत में स्थित हो जाए। जैसे अग्नि अपने आश्रय वस्तु के भस्म हो जाने पर शांत होकर स्वरूप में स्थित हो जाती है, वैसे ही वह आत्मा भी पूर्ण विरक्ति और समाधि में स्थित होकर परम शांति को प्राप्त हो।
नारदजी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज! यदि वानप्रस्थी में ब्रह्मविचार की सामर्थ्य हो, तो वह शरीर को छोड़कर बाकी सब त्यागकर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर ले। संन्यासी को न व्यक्ति, न वस्तु, न स्थान और न ही समय की कोई अपेक्षा रखनी चाहिये। उसे केवल एक गाँव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करना चाहिये।
यदि वह वस्त्र धारण करे, तो केवल कौपीन धारण करे। और जब तक कोई विशेष आपत्ति न आये, तब तक अपने आश्रम-चिह्नों और दण्ड के अलावा किसी त्यागी वस्तु को न अपनाये।
संन्यासी को चाहिए कि वह शान्तचित्त, भगवत्परायण, सब प्राणियों का हितैषी और आत्मरति होकर अकेले विचरण करे—किसी भी सांसारिक आश्रय पर निर्भर न रहे। वह इस सृष्टि में ब्रह्म का अनुभव करे। ऐसा संन्यासी अनुभव करता है और जानता है कि बंधन और मोक्ष दोनों ही माया हैं—वास्तव में इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। संन्यासी न तो मृत्यु का स्वागत करे, न जीवन की कामना। जीवनयापन के लिए कोई आजीविका न अपनाये, केवल तर्क-वितर्क के लिए शास्त्र चर्चा न करे और संसार में किसी भी विचारधारा का पक्ष न ले। वह शिष्य समूह न बनाये, ग्रंथों का भारी अभ्यास न करे, न प्रवचन दे और न ही कोई बड़ा आयोजन आरम्भ करे। ऐसा शान्त, समदर्शी, महात्मा संन्यासी किसी विशेष आश्रम के चिह्नों से बंधा न हो। चाहे वह उन चिह्नों को धारण करे या त्याग दे, उसे उससे कोई अन्तर नहीं। उसके पास कोई बाहरी आश्रम-चिह्न न हो, लेकिन वह भीतर आत्मानुसन्धान में सदा मग्न रहे। वह अत्यंत विचारशील हो, परंतु संसार को वह बालक, पागल या मूक जैसा प्रतीत हो। वह प्रतिभाशाली होते हुए भी साधारण लोगों की दृष्टि में निर्बुद्धि जान पड़े—ऐसा संन्यासी सच्चे आत्मदर्शन की ओर अग्रसर होता है।
नारदजी युधिष्ठिर को इस विषयमें एक प्राचीन इतिहासका वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रह्लादका संवाद।
दत्तात्रेय द्वारा प्रह्लाद को संतोष एवं वैराग्य संबंधी उपदेश
एक बार भक्त शिरोमणि प्रह्लादजी लोकों में भ्रमण कर रहे थे ताकि वे जान सकें कि लोगों के हृदय में क्या चल रहा है। सह्याद्रि पर्वत की तलहटी में, कावेरी नदी के तट पर, उन्हें एक दिव्य पुरुष भूमि पर पड़े दिखाई दिए। वे बाहर से धूल-धूसरित और सामान्य दिखाई दे रहे थे, परन्तु उनके शरीर से तेजस्विता झलक रही थी। लोग उनके शरीर, वाणी या कर्म से यह नहीं पहचान पा रहे थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं। परन्तु प्रह्लादजी ने अपने दिव्य भाव से समझ लिया की वह भगवान दत्तात्रेय हैं और उनके चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया। पूजा करके उन्होंने नम्रता से पूछा — “भगवन! आप कर्म नहीं करते, भोग भी नहीं करते, फिर भी आपका शरीर हृष्ट-पुष्ट कैसे है?”
दत्तात्रेयजी मुस्कराकर बोले, “हे प्रह्लाद! तुम तो खुद जानते हो कि कर्म करने से क्या फल मिलता है और कर्म से हटने से क्या लाभ होता है। तुम्हारी भक्ति के कारण भगवान नारायण हर समय तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। फिर भी, तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ।
तृष्णा (इच्छा) एक ऐसी चीज़ है जो पूरी कभी नहीं होती, चाहे मनुष्य को कितने भी भोग क्यों न मिल जाएँ। इसी तृष्णा ने मुझे जन्म-मरण के चक्कर में डाल दिया। मैं न जाने कितने काम करता रहा, और उन कर्मों के कारण न जाने कितनी योनियों में जन्म लिया। अब इस जन्म में मुझे मनुष्य शरीर मिला, जो बहुत दुर्लभ है — अगर पुण्य करूँ तो स्वर्ग मिल सकता है, पाप करूँ तो जानवर की योनि, त्याग करूँ तो मोक्ष और अगर मिला-जुला कर्म करूँ तो फिर मनुष्य जन्म। मैंने देखा कि लोग सुख पाने और दुःख मिटाने के लिये बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको और दुःख ही मिलता है। इसी कारण मैंने सब कर्म छोड़ दिये। सच्चा सुख आत्मा में है। जब मन की सारी चेष्टाएँ रुक जाती हैं, तब वह आत्मा प्रकट होती है। इसलिए अब मैं जैसा कुछ प्रारब्ध से मिलता है, उसी में पड़ा रहता हूँ।
मनुष्य अपने असली सुख को भूलकर, बाहर के भोगों में सुख ढूँढता है। लोग आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ते हैं। शरीर और उसका सुख-दुःख तो प्रारब्ध के अधीन है। जो मनुष्य शरीर के माध्यम से सुख पाना चाहता है, वह सफल नहीं होता। अगर कोई बहुत मेहनत से धन या सुख भी पा ले, तो भी चैन नहीं मिलता। धनवान लोग हर समय डर और शक में रहते हैं। जो जीवन और धन से बहुत मोह रखते हैं, वे हर किसी से डरते हैं — राजा, चोर, दुश्मन, अपने रिश्तेदार, पशु-पक्षी, भिखारी, समय और यहाँ तक कि खुद से भी। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसे मोह का त्याग करे, जो हमें शोक, मोह, भय, क्रोध और थकावट देता है।
मेरे दो गुरु – मधुमक्खी और अजगर हैं। मधुमक्खी ने मुझे सिखाया कि जैसे वह मेहनत से शहद इकट्ठा करती है लेकिन कोई दूसरा आकर उसे छीन लेता है — वैसे ही धन का संग्रह व्यर्थ है। अजगर से मैंने सिखा कि जैसे वह बिना किसी प्रयास के पड़ा रहता है, और जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है- वैसे ही जीवन जीना चाहिए।
मैं कभी थोड़ा खाता हूँ, कभी ज़्यादा; कभी स्वादिष्ट, कभी बेस्वाद; कभी दिन में, कभी रात में; कभी एक बार, कभी दो बार। कभी रेशम के वस्त्र पहनता हूँ, कभी चीर-वल्कल। कभी ज़मीन पर सोता हूँ, कभी गद्दे पर। कभी महलों में घूमता हूँ, कभी बिलकुल नग्न पिशाच जैसा। मैं न किसी की निंदा करता हूँ, न प्रशंसा। मैं बस चाहता हूँ कि सबको परमात्मा से मिलन हो।
सत्य खोजने वाले को चाहिए कि यह जो भिन्न-भिन्न चीज़ें दिख रही हैं, उन्हें अपने मन की वृत्तियों में हवन कर दे। मन को बुद्धि में, बुद्धि को अहंकार में, अहंकार को महत्तत्त्व में और सबको अंत में माया मानकर आत्मज्ञान में स्वाहा कर दे। जब यह सब हो जाता है, तब आत्मा में स्थित हो जाओ — शांत, स्थिर और कर्मों से उपराम।
हे प्रह्लाद! यह आत्मकथा बहुत गुप्त है, शास्त्रों से भी ऊपर की बात है। पर तुम नारायण के प्यारे हो, इसलिए मैंने यह तुम्हें सुनाई।
नारदजी कहते हैं की जब प्रह्लादजी ने दत्तात्रेयजी से यह ज्ञान सुना, तो उन्होंने श्रद्धा से उनकी पूजा की और प्रसन्न होकर अपनी राजधानी की ओर लौट गये।
सारांश: JKYog India Online Class- श्रीमद् भागवत कथा [हिन्दी]- 23.05.2025