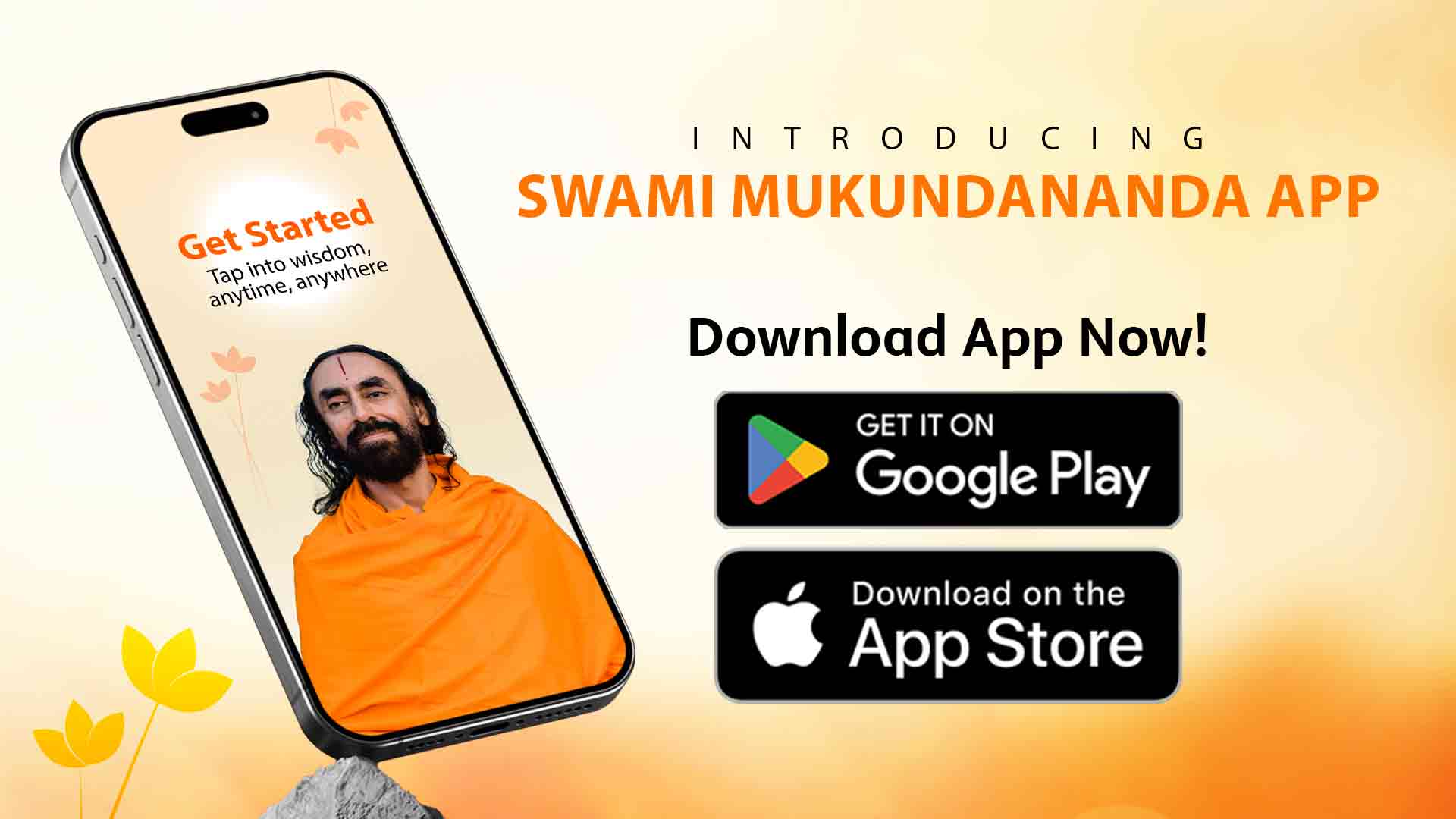कठ उपनिषद् - सत्र सारांश – ७
व्याहृतियों की उपमा से अनात्मा एवं परमात्मा का भेद समझाना
नचिकेता का तीसरा वरदान इतना महत्त्वपूर्ण है कि स्वयं यमराज भी इस वरदान को पूरा करने में अपना उत्साह व्यक्त कर रहे हैं। यही कारण है कि वे परमेश्वर को विभिन्न उपमाओं से, द्रष्टांतों से तथा सिद्धांतों से समझा रहे हैं। उनका यह ज्ञान उनके यमपदारूढ़ होने की योग्यता को भी दर्शाता है।
‘परमात्मा’ के अनुभव को अधिक स्पष्ट करने के लिए अब वे ‘अनात्मा’ से उसकी तुलना करते हैं। एवं, उर्ध्व जगत की व्याहृतियों में होने वाले ज्ञानात्मक अनुभवों के आधार पर वे नचिकेता को समझाते हैं कि –
जैसे स्वच्छ दर्पण में ही प्रतिबिंब दीखता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण से ही ब्रह्म को धारण किया जाता है। जैसे स्वप्न में वस्तुएँ भासती हैं, वैसे ही पितृलोक में भगवान् भासते हैं। जैसे जल में वस्तुएँ प्रतिबिंबित होती हैं, वैसे ही गन्धर्वलोक में भगवान् की झलक-सी मिलती हैं। अंततः, ब्रह्मलोक में तो छाया व धूप की भाँति अनात्मा एवं परमात्मा, जीवात्मा को स्पष्ट अनुभव में आने लगते हैं।
- तात्पर्य, भू: एवं भुवः व्याहृतियों के अन्तर्गत आनेवाले मृत्युलोक, द्युलोक, चंद्रलोक एवं पितृलोक में जीवात्मा का ज्ञान अधिकाँश इन्द्रिय-प्रधान ही होता है। यद्यपि, भूलोक से पितृलोक तक जाते-जाते उस ज्ञान में शुद्धता बढ़ती जाती है; किन्तु वह ऐन्द्रिक विषयों के आसपास ही सीमित रहता है। अतः भूलोक से पितृलोक तक भगवान् का जो ज्ञान होता है वह अधिकांश सकाम एवं इन्द्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के आसपास ही केन्द्रित होता है।
- गन्धर्व लोक से जीव की चेतना ऐन्द्रिक भोगों से ऊपर उठ कर, कला-सम्पादन की ओर आगे बढ़ती है। आनंद-मीमांसा के इस स्तर से, जीव अपने भोगों को विकसित करने पर कम ध्यान देता है तथा अपने अस्तित्व के प्रभाव को विकसित कर उसे दूरोगामी बनाने की ओर अग्रसर होता है। गन्धर्व लोक से स्वः व्याहृति के अन्त तक, इन्द्रलोक तक, जीव अपने प्रभाव को विकसित करने हेतु भिन्न-भिन्न कलाएँ तथा विद्याएँ प्राप्त करने में जुटा रहता है। अतः, इस व्याहृति में जीव का भगवान् विषयक ज्ञान कला-प्राप्ति एवं विद्या-प्राप्ति की सकामता से ग्रस्त रहता है।
- पश्चात्, महर्लोक से ब्रह्मलोक तक जीव यही अन्वेषण में ही डूबा रहता है कि वह अपने स्वरूप को स्पष्ट कर के, ब्रह्माण्ड में अपने अस्तित्व को रचयिता के लिए कैसे उपयुक्त कर सकता है। यह अन्वेषण करते-करते जीव जब इतना योग्य हो जाता है कि वह ब्रह्मलोक में गति प्राप्त कर सकता है, तब उसका अनात्मा तथा परमात्मा के सन्दर्भ में ज्ञान इतना स्पष्ट हो चूका होता है कि वह केवल भगवत्प्राप्ति की ही इच्छा रखता है; अन्य किसी भी सिद्धि, उपलब्धि या विद्या को नहीं चाहता। वह केवल ब्रह्मविद्या को ही चाहता है जिससे की वह माया से उत्तीर्ण हो सके। और यदि वह जीव इस एकमात्र लक्ष्य से हट जाता है तो आब्रह्मभुवनाल्लोकाः के अनुसार वह पतन-प्राप्त हो कर, पुनः मृत्युलोक की रजोगुणी योनि में लौट आता है।
भोगों के प्रति उपरामता का उपदेश
भगवत्प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम मनुष्य को भोगों से उपराम होना पड़ता है। तभी वह अपनी कर्म-शक्ति का यथायोग्य उपयोग कर के भगवदीय चेतना को विकसित कर सकता है एवं अन्यों में प्रसारित कर सकता है। अतः अब नचिकेता को उस उपरामता के विषय में समझाते हुए यमदेव ने कहा –
अपने-अपने कारण से भिन्न-भिन्न रूपों में उत्पन्न हुई इन्द्रियों की जो पृथक्-पृथक् सत्ता है; और जो उनका उदय-लय होने का स्वभाव है; उसे जानकर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करते। (इन्द्रियाणां पृथक् भावम्)
- योगी की जिजीविषा का यही स्वरूप होता है कि वह भोग के लिए नहीं अपितु योग के लिए अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहता है। अतः एक कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी या भक्तियोगी यह बात भलीभाँति समझे रहता है कि इन्द्रियाँ अपनी-अपनी तन्मात्राओं से उत्पन्न होती हैं एवं उन तन्मात्रा से जुड़े हुए पञ्च-महाभूत के विषय की इच्छा करती है। यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसके स्पंदनों को मन के द्वारा नियमित व अनुभूत किया जाता है। अतः ऐसे परिणामी ऐन्द्रिक विषय जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकते – यह विचार कर वह भोगों की नित्यता को देख कर, सहज ही भोगों के प्रति उपराम हो जाता है।
व्यक्त इन्द्रियों से अव्यक्त अलिंग पुरुष की ओर
जीव जब भोगों से उपराम हो जाता है तब वह तीव्र गति से उस परम अव्यक्त परब्रह्म की ओर गति करता है। अतः अब व्यक्त संसार से अव्यक्त की ओर होनेवाली गति का दार्शनिक निरूपण करते हुए यमराज नचिकेता को कह रहे हैं कि –
- इन्द्रियों से मन श्रेष्ठ है।
- मन से उत्तम है – सात्विक बुद्धि (प्रज्ञा)।
- उस बुद्धि से परे (महान) है उसका स्वामी – आत्मा।
- आत्मा से अधिक शक्तिशाली है अव्यक्त शक्ति – माया।
- परंतु, अव्यक्त माया से भी अधिक व्यापक वह अलिंग परमपुरुष श्रेष्ठ है। उस ब्रह्म को जानकर जीवात्मा माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान् के अमृतमय संसार में नित्यकालीन प्रवेश प्राप्त कर लेता है।
- हे नचिकेता! जब मनसहित पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ भलीभाँति अपने आधार में स्थिर हो जाती हैं; और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती; उस स्थिति को योगी ‘परमगति’ कहते हैं। (मायोपधिक परम गति)
- वस्तुतः तो यह आत्मज्ञान की ही स्थिति है – ब्रह्मज्ञान की नहीं। फिर भी, योगी उसे ‘परम गति’ के समान अनुभव करता है। क्योंकि, इससे पूर्व इतना शांत व निर्गतियुक्त मन उसने अनुभव नहीं किया होता। अतः मन की संसार की ओर भागने की गति रुकने पर उसे आत्मा के नित्य आनंद का आभास मिलता है। यह आनंद माया की ही उपाधि से, संयोग से, मिलता है। इसलिए इसे ‘मायोपाधिक’ कहा गया है।
- उस इन्द्रियों की स्थिर धारणा को ही ‘योग’ माना गया है। क्योंकि, उस समय साधक प्रमादरहित हो जाता है। किन्तु, यह योग स्वभावतः उदय-अस्त होनेवाला है। (योगो हि प्रभवाप्ययौ)
- आत्मज्ञान में स्थिति नित्य नहीं रह सकती। क्योंकि, योगी स्व-प्रयत्न से मन की गति को तो रोक लेता है; किन्तु कारण-शरीर के अनंत संस्कारों का वेग रोकना उसके लिए तब तक असंभव ही रहता है जब तक वह स्वयं अनंत परब्रह्म से जुड़ नहीं जाता।
- इसी कारण-शरीर के संस्कारों के वेग से, उसकी समाधि में पहले जो उत्थान हुआ था उसमें कुछ अवधि बाद व्यवधान होने लगता और वह पतन को प्राप्त होता है। इसी उत्थान को यमराज ने यहाँ ‘प्रभव’ कहा है; और पतन को ‘अप्यय’।
भगवत्प्राप्ति में दृढ़ विश्वास का महत्त्व
भगवान् से योग करने की, अर्थात्, भगवत्प्राप्ति करने की साधना में यदि उपर्युक्त प्रभव और अप्यय आते रहेते हैं तो साधक का मन विचलित हो कर निराश होने लगता है। अतः इस समय साधक को धैर्य से काम लेना पड़ता है और अपने मन में भगवत्प्राप्ति के विश्वास को सुस्थिर बनाए रखना पड़ता है। यही बात को उजागर करते हुए, यमदेव उत्साहवर्धक उपदेश देते हुए नचिकेता से कहते हैं कि –
वह परब्रह्म परमेश्वर न तो वाणी से न मन से न नेत्रों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। किन्तु, “वह अवश्य ही प्राप्तव्य है।” ऐसा दृढ़ विश्वास रखनेवालों के अतिरिक्त वह अन्य किसे मिल सकता है! (अस्ति इति; तत् उपलभ्यते)
अतः प्रयत्नशील मुमुक्षु को चाहिए कि पहले तो, “वह अवश्य प्राप्तव्य है” – ऐसा भगवान् में अस्तित्व-भाव दृढ़ करे। तदनन्तर, तत्त्वज्ञान से माया के समस्त अभावों के आकर्षण का ही अभाव कर देना है। इस प्रकार, तत्त्वभाव को सिद्ध कर के ही परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्रसन्न करना है। (अस्तीत्येवोपलब्धव्यः; अस्तीत्येवोपलब्धस्य)
भगवत्प्राप्ति की यात्रा में होने वाले चार प्रकार के ‘अभाव’ की दार्शनिकता
भगवान् ही परम ‘भाव’ (अस्तित्व) है। अतः हमारे सारे मनोभाव उन्हीं की ओर बहने लगें यही वास्तविक भक्ति है। इस प्रकार, जब हम भगवान् की ओर जाने लगते हैं तब अनर्थों कि निवृत्ति होने लगती हैं और भगवत्प्राप्ति में अनुकूल हो ऐसे भिन्न-भिन्न ‘अभावों’ का उदय होने लगता है। इसी दार्शनिकता का उद्घाटन करते हुए यमदेव ‘अन्तक’ ने नचिकेता से कहा –
भगवत्प्राप्ति में पूर्वोक्त दृढ़ विश्वास करने से साधक के हृदय में स्थित आकर्षणों की समस्त कामनाओं का अत्यंत अभाव हो जाता है। तब वह मरणधर्मा संसार का अतिक्रमण कर के अमृत को प्राप्त कर लेता है। तथा, यहीं – इसी शरीर में परब्रह्म का भलीभाँति अनुभव कर लेता है। (हृदि श्रिताः कामाः प्रमुच्यन्ते; अमृतो भवति; अत्र ब्रह्म समश्नुते)
- यहाँ भगवत्प्राप्ति होने पर कामनाओं का ‘अत्यंत अभाव’ होना कहा गया है। यह चार प्रकार के अभावों में से सब से अन्त में होने वाला अभाव है। वह चार अभाव इस प्रकार है –
1. प्राग् अभाव – कारण से उत्पन्न होने से पूर्व (प्राग्) कार्य का अभाव होना। जैसे, बीज से उत्पन्न होने के पूर्व उसमें निहित फूल का अभाव ही था।
- यमराज ने महाभूतों में से इन्द्रियों की उत्पत्ति की जो बात कही है वह महाभूतों की अपेक्षा इन्द्रियों का पाग् अभाव ही है।
2. प्रध्वंस अभाव – कार्य का नाश (ध्वंस) होने पर उसका अभाव होना। जैसे, फूल को पतझड़ की ऋतु में मूल द्वारा पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण उस फूल का ऋतुनाश हो जाता है।
- यमराज ने मनसहित ज्ञानेन्द्रियों का प्रज्ञा में स्थित हो जाना एवं प्रज्ञा का धारणा में स्थित होना कहा है वह इन्द्रिय-मन-बुद्धि का धारणा में होने वाला प्रध्वंस अभाव ही है।
3. अन्योन्य अभाव – एक कार्य का दूसरे कार्य से भिन्न होना। जैसे, बीज में पत्थर का अभाव होना एवं पत्थर में बीज का अभाव होना।
- यमराज ने इन्द्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, आत्मा से माया और माया से भगवान् के श्रेष्ठ होने की जो बात कही है उसमें कार्यप्रणाली के दृष्टिकोण से, इन्द्रियों का मन से अन्योन्य अभाव है। इसी प्रकार, मन का बुद्धि से, बुद्धि का आत्मा से, आत्मा का माया से, माया का भगवान् से अन्योन्य अभाव है। तात्पर्य, उनकी कार्यप्रणाली आपस में एकदूसरे से बिलकुल भिन्न है।
4. अत्यंत अभाव – कार्य-कारण का काल-अबाधित अंत (अति अंत) होना। जैसे, बीज को जला देने पर उसमें सूक्ष्म रूप से स्थित पर्ण, फल, फूल एवं अन्य बीज सदा के लिए अभाव को प्राप्त हो जाते हैं।
- यमराज ने भगवत्प्राप्ति होने पर मायिक आकर्षणों का नित्य अभाव होना कहा है वह उनका अत्यंत अभाव है। पुनः माया के आकर्षण उस भगवत्प्राप्त महापुरुष को त्रिकाल में भी परास्त नहीं कर सकते।
मायाबद्ध जीव की गत्यागति एवं मुक्ति का वर्णन
नचिकेता को अपना अंतिम उपदेश दे कर समापन करते हुए यमलोकाधिपति ‘अन्तक’ ने कहा –
जीव के हृदय की कुल मिलाकर एक सौ एक नाड़ियाँ हैं। उनमें से एक, सुषुम्णा नाड़ी, मूर्धा की ओर निकली हुई है। उसके द्वारा मनुष्य, उर्ध्वलोकों में जा कर, अमृत का पान करता हैं। अन्य एक सौ नाड़ियाँ मनुष्य को मरणकाल में विषम योनियों में गति देने में हेतु बनती हैं।
- जब जीव की भगवत्प्राप्ति होती है तब उसकी भोगों के प्रति उपरामता हो जाती है। अतः पहले जो नाड़ियाँ उसे भोगों में रत रख रहीं थीं वे – इडा एवं पिंगला – नाडीयों की समस्त ऊर्जा अब, भोगोपरामता के कारण, एकजूट हो कर सुषुम्णा नाड़ी में चली जाती है। इस समय जीव की प्राण-शक्ति इतनी बलवान हो जाती है कि वह समस्त कुण्डलिनी-मंडल का भेदन कर के मूर्धा के माध्यम से शरीरत्याग कर देता है।
- किन्तु, यदि वह भगवत्प्राप्ति के संकल्प पर दृढ़ नहीं रहता तो इडा और पिंगला नाडीयों के भोगपरक व्यवहार उसे जन्म-मरण के चक्रों में आबद्ध करते ही रहते हैं; जब तक की उसकी भगवत्प्राप्ति नहीं हो जाती।
सब का अन्तर्यामी, अंगुष्ठमात्र परिमाणवाला परमपुरुष, सदैव जीवों के हृदय में भलीभाँति प्रविष्ट हैं। उसको मूँज से सींक की भाँति आत्मा से तथा शरीर से धैर्यपूर्वक पृथक् कर के देखो। उसी को विशुद्ध अमृतस्वरूप समझो। हाँ, केवल उसी को ही विशुद्ध अमृतस्वरूप समझो। (तं विद्यात् शुक्रम् अमृतम्।)
इस प्रकार उपदेश-श्रवण कर के, नचिकेता ने मृत्युदेव यमराज के द्वारा बतलायी हुई इस विद्या को और संपूर्ण योग की विधि को प्राप्त कर के, मृत्यु से रहित हो कर तथा सब प्रकार के विकारों से शून्य विशुद्ध हो कर, ब्रह्मभाव (भगवत्प्राप्ति का सुदृढ़ निश्चय) प्राप्त कर लिया। तथा, अन्य जो कोई भी इस अध्यात्मविद्या को नचिकेता की भाँति ग्रहण करेगा, वो भी अवश्य भगवत्प्राप्ति करने के सुदृढ़ निश्चय को ही प्राप्त होगा।
इस प्रकार, मृत्यु के देवता ने नचिकेता के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को मृत्यु से पार हो कर, भगवत्प्राप्ति करने का सुन्दर मार्ग व सिद्धांत प्रस्तुत किए।
परमहंस नचिकेता एवं भगवान् के प्रतिनिधि मृत्युदेव यमराज के चरणों में सादर सहस्त्रशः वंदन..!
॥ इति कठ उपनिषद् ॥
॥ इति कठ उपनिषद् ॥
जय जय श्री राधे! जय जय श्री राधे!! जय जय श्री राधे!!!
सारांश: JKYog India Online Class- उपनिषद सरिता [हिन्दी]- 1.10.2024