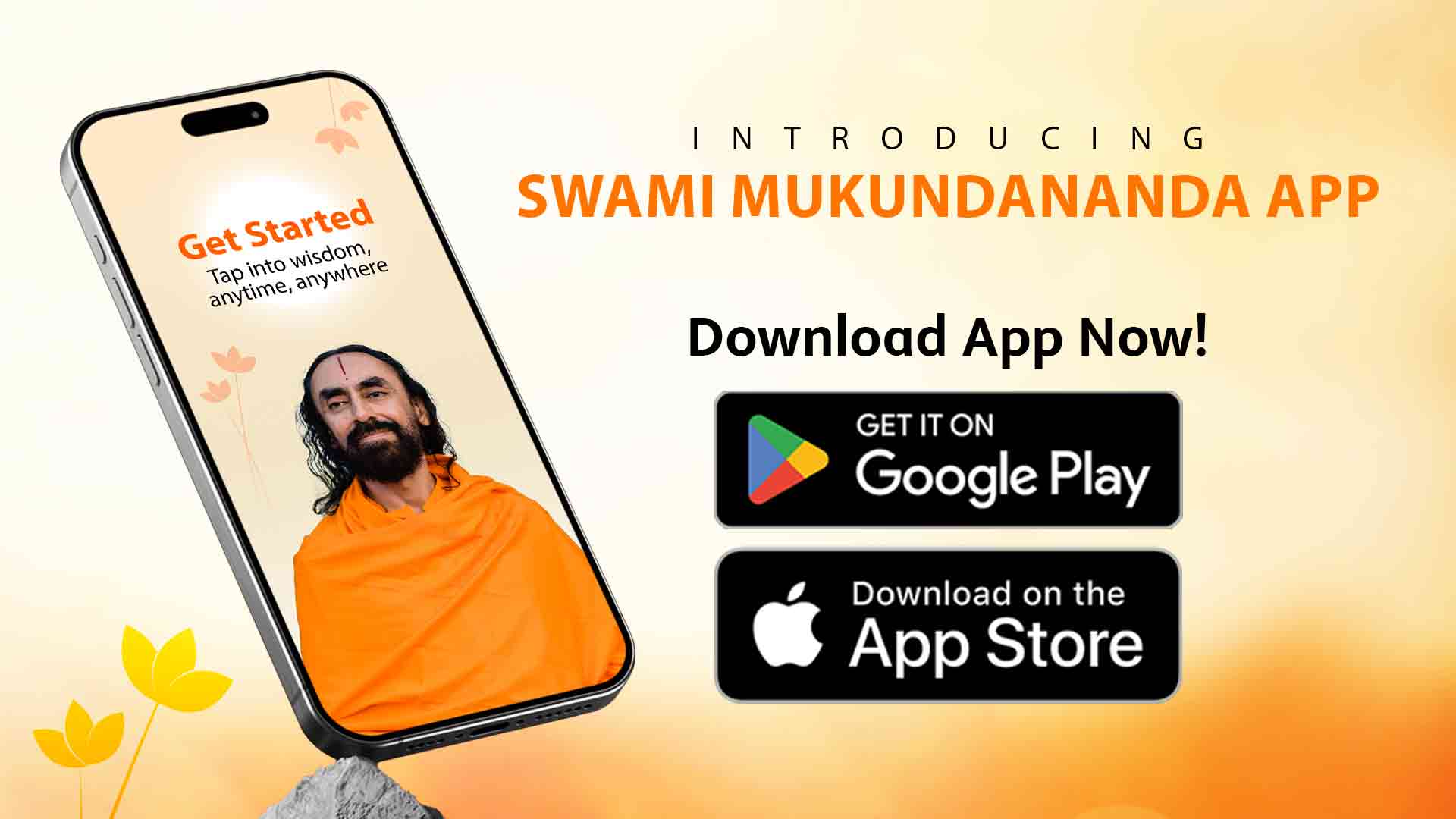कठ उपनिषद् - सत्र सारांश – ५
आत्मस्थ परमात्मा का ‘अवक्रचेतस’ स्वरूप
जिज्ञासु ब्राह्मण बालक नचिकेता को परमात्म-तत्त्व का उपदेश देते हुए यमराज ने कहा:
“अजन्मा ‘अवक्रचेतस’ आत्मा का एकादश द्वारों वाला एक नगर है। इसी पुर में रहते हुए परमेश्वर का अनुष्ठान-साधन (उपासना) कर के जीव शोकमुक्त व जीवनमुक्त हो कर अंततः मायामुक्त हो जाता है। ऐसा है वह परम तत्त्व।”
- बद्ध जीवात्मा को ‘वक्रचेतस’ कहा जाता है; क्योंकि संसार में रमण करने के लिए जीव की ज्ञानवान और शाश्वत चेतना विजातीय, जड़ और नश्वर, शरीर-इन्द्रिय-मन-बुद्धि में व्याप्त हो कर वक्रता को प्राप्त हो कर, संसार से तादात्म्य कर लेती है। इसी तादात्म्य को ‘अध्यास’ (आवरण) कहते हैं।
- ऐसा यह जीवात्मा स्वरूप से मायारहित होने से भगवान् के समान ही ‘अवक्रचेतस’ है। वह जीव एकदाश द्वार वाले नगर रूपी इस मानव शरीर में निवास करता है।
वह एकादश द्वार में से नौ द्वार स्थूल शरीर में हैं: दो आँखें; दो नासिका, दो कान, मुख, गुदा, उपस्थ (जननेन्द्रिय)।
दसवाँ द्वार सूक्ष्म शरीर में है, जो ‘नाभि’ है। नाभि से ही जीव के इस शरीर के तार जुड़े होते हैं जिसे यमदूत मृत्यु के समय काट कर जीव को इस शरीर से विलग कर के अन्यत्र ले जाते हैं। तदुपरांत; योगिक विद्याओं को स्थिर करने हेतु प्राणों को रोकने के लिए भी इस नाभि के सूक्ष्म छिद्र का उपयोग होता है; जिसे योगी ‘नाभि-चक्र’ कहते हैं; जो ‘स्वाधीष्ठान’ कुण्डलिनी चक्र से भिन्न होता है।
ग्यारहवाँ द्वार कारण शरीर से संयुक्त होता है, जो ब्रह्म-रंध्र है। मस्तक में शिखा रखने का वह स्थान जो थोड़ा मृदु होता है; उसे मूर्धा कहते हैं। इस मूर्धा का उद्गम स्थान कारण शरीर में होता है; अतः वहाँ तक यह छिद्रयुक्त होती है। इसी उद्गम स्थान को ‘ब्रह्म-रंध्र’ कहते हैं। योगिक विद्याओं की संपूर्ण सिद्धि होने पर जीव जब मुक्त होता है तब इसी ब्रह्म-रंध्र से प्राणों के वेग के साथ वह बाहर निकलता है।
इस पवित्र एकादश द्वारों वाले नगर में रह कर उस जीव का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर की उपासना रूपी अनुष्ठान में व्यस्त रहें एवं उनकी सृष्टि में भगवत्चेतना का प्रसार करें। ऐसा करने पर जीव शोकमुक्त व जीवनमुक्त हो कर अंततः मायामुक्त हो कर, भगवान् के धाम में प्रवेश कर जाता है।
परम तत्त्व ऐसा कल्याणमय है! (एतद्वै तत्।)
सृष्टि से स्रष्टा की ओर
इन्द्रियों की संसार के प्रति सन्मुखता होने के कारण, सृष्टि के आयामों का ही अवलंबन ले कर, मृत्युदेव अन्तक अब स्रष्टा (परब्रह्म) का वर्णन करते हुए नचिकेता से कहते हैं –
१. वह परमब्रह्म अत्यंत पवित्र परम धाम (शुचिपद) में रहने वाला एकमात्र ‘हंस’ (धामी) है।
२. वही अंतर्मन में दर्शन (ईक्षण) किये जाने वाले अंतरीक्ष में निवास करने वाला वसु रूपी शाश्वत तत्त्व है।
३. वह परब्रह्म दहराकाश रूपी गृह (दुरोण) में रहनेवाला समयातीत, तिथिरहित (अतिथि) तत्त्व है।
४. परमेश्वर ही शरीररूपी वेदि पर स्थापित (वेदिषद्) ऊर्जास्त्रोत के रूप में प्रकट अग्नि है।
५. उस वेदि के आधार पर होने वाले यज्ञों (कर्मों) के लिए आवश्यक आहुति (प्राण) प्रदान करने वाला ‘होता’ भी वही परमेश्वर है।
६. वह परब्रह्म समस्त जीवों में रहने वाला (नृषत्) है; तथा उनको पोषित करने वाले वरद देवताओं में भी निवास करनेवाला (वरसत्) है।
७. वह परात्पर संसार में सर्वव्यापक रूप में रहने वाला (व्योमसत्) है।
८. परमेश्वर ही इन्द्रियों में एवं उसकी तन्मात्राओं में प्रकट होने वाला (गोजाः) है।
९. वह आदि तत्त्व ही भवसागर के जल (महान् तत्त्व) को प्रकट करने वाला (अब्जाः) है।
१०. अविद्या के घने बादलों (अद्रि) को प्रकाशित करने वाले विद्युत (अद्रिजाः) के रूप में परब्रह्म ही सत्ताशील है।
११. सृष्टि के विधान (ऋत्) में क्रियान्वित रहने वाला (ऋतसत्), उन विधानों के परिणामों के रूप में प्रकट होने वाला (ऋतजाः) एवं तमाम विधानों का अंतिम विभु-विधान (वृहत् ऋतम्) वही परात्पर परमेश्वर है।
मृत्युनियंता के द्वारा परमात्म-तत्त्व की अद्वितीयता का वर्णन:
वह परब्रह्म शरीर के मध्य हृदयासीन होते हुए ही, प्राण को ऊपर की और उठाता है एवं अपान को नीचे धकेलता है। वह सर्वश्रेष्ठ (वामन) भजनीय परमात्मा की विश्व-संचालक देवतागण भी उपासना करते हैं। हे मनुष्यों! वही परमेश्वर का तुम भी भजन करो।
- यहाँ ‘वामन’ शब्द का अर्थ है – जिसकी महिमा के आगे अन्य सभी सहज ही वामन (सामर्थ्य में लघु) सिद्ध हो वह।
वर्तमान शरीर में स्थित तथा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रयाण करनेवाला जीवात्मा जब इस शरीर से निकल जाता है, तब यहाँ इस शरीर में क्या शेष रह जाता है!? वही है वह परब्रह्म, जिसके विषय में, नचिकेता, तुमने पृच्छा की है । (एतद्वै तत्।)
- क्योंकि, मृत्यु के समय जब जीव शरीर का त्याग करता है तब उसके साथ जीवस्थ परमात्मा भी प्रयाण कर जाते हैं। पश्चात्, मृत शरीर में सर्वव्यापक परमेश्वर का ही प्रभाव रह जाता है। उनके प्रभाव से ही वह मृत मायिक शरीर के पञ्च-तत्त्व माया के पञ्च-महाभूत में विघटित हो जाते हैं।
अपने-अपने कर्मों के अनुसार एवं शास्त्रों के श्रवण या अश्रवण के द्वारा नाना योनियों में प्रविष्ट होने वाले जीवों के लिए नाना भोगों का निर्माण करनेवाला परम पुरुष प्रलयकाल में सब के सो जाने पर भी जागता रहता है। वही परम विशुद्ध तत्त्व अमृतमय ब्रह्म है। सृष्टि के समय, उसी में सारे लोक आश्रित हो रहे होते हैं। उसका कोई अतिक्रमण नहि कर सकता। वही है वह परब्रह्म। (एतद्वै तत्।)
- शास्त्रों के श्रवण का आदर कर के जीवन में अनुशीलन करना ही वास्तविक ‘श्रवण’ माना जाता है। केवल कानों से सुन कर पश्चात् मन-माना जीवन ही जीना हो तो वह केवल कान से सुना हुआ श्रवण भी वस्तुतः ‘अश्रवण’ ही माना जाता है।
- यदि वास्तविक श्रवण किया है तो जीव को उन्नत सद्गति मिलती है। यदि अश्रवण किया है तो वह जीव हठात् अधोगति की ओर ही जाएगा।
- प्रलय के बाद संपूर्ण विश्व को अपने भीतर बीजरूप में समाहित करने पर सारे जीव भगवान् के महोदर में चिर-निद्रा में चले जाते हैं; किन्तु भगवान् स्वयं अपने निजानंद में जागते ही रहते हैं। जब उनमें ह्लादिनी शक्ति का वेग तीव्र होता है तो पुनः वे जीवों के प्रति करुणित हो कर उन्हें सृष्टि के साथ प्रकट कर देते हैं।
इस प्रकार, नचिकेता के परम-तत्त्व विषयक तीसरे वरदान को पुष्ट करते हुए यमराज ने नचिकेता को परमेश्वर की अद्वितीयता एवं उनकी आत्मा में अन्तर्यामीता से भलीभाँति अवगत करा दिया।
सारांश: JKYog India Online Class- उपनिषद सरिता [हिन्दी]- 17.09.2024